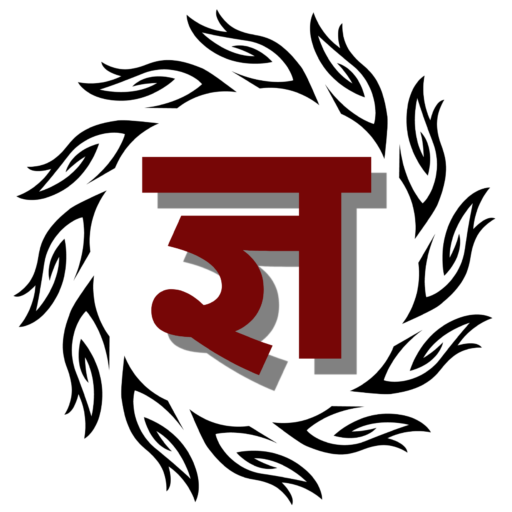भूमिका
साँची प्रस्तर लेख मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद में स्थित साँची महास्तूप के पूर्वी द्वार के दक्षिण बीच की वेदिका की चौथी पंक्ति तथा कोने के भाग में अंकित है। इसको कैप्टेन एडवर्ड स्मिथ ने ढूँढ निकाला था और जेम्स प्रिंसेप ने उसका पाठ और अनुवाद प्रकाशित किया। तत्पश्चात् जे० एफ० फ्लीट ने अपने Corpus Inscriptionum Indicarum में इसे सम्मिलित किया।
संक्षिप्त परिचय
नाम :- साँची प्रस्तर लेख
स्थान :- साँची, रायसेन जनपद, मध्य प्रदेश
भाषा :- संस्कृत
लिपि :- ब्राह्मी
समय :- गुप्त सम्वत् १३१ ( ४५०-५१ ई० ), कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल
विषय :- हरिस्वामिनी द्वारा १२ दीनार का अक्षयनीवी दान
मूलपाठ
१. सिद्धम्। उपासक सनसिद्ध भार्य्यया उपासिका हरिस्वामिन्या-
२. माता पितरमुद्दिश्य काकनादबोट महाविहारे चातुर्द्दिशयार्य्य सं-
३. घाय अक्षयनीवी दत्ता दीनारा द्वादश [।] एषां दीनाराणां या वृद्धि-
४. रूप जायते तथा दिवसे संघमध्यप्रविष्ठकभिश्ररैकः भोज-
५. यितव्यः [॥] रत्नगृहेऽपि दीनार त्रयदत्तं [।] तद्दीनार त्रयस्य वृद्ध्या
६. भगवतां बुद्धस्य दिवसे दिवसे दीपत्रयं प्रवालित्यं [॥] चतुर्बुद्धास-
७. नेऽपि दत्तः दीनार एकः [।] तस्य वृद्ध्या चतुर्बुद्धासने भगवतो बुद्धस्य
८. दिवसे-दिवसे दीपः प्रवालयितव्यः [॥] एवमेषाक्षयनीवी-
९. आचन्द्रार्कशिलालेख्या स्वामिनीसनसिद्धभार्य्यया
१०. उपासिका हरिस्वामिन्या प्रवार्तिता इति [॥]
११. संव्वत् १००[+]३०[+]१ अश्वयुग्दि ५ ॥
हिन्दी अनुवाद
सिद्धि प्राप्त हो। उपासक सनसिद्ध की पत्नी उपासिका हरिस्वामिनी ने अपने माता-पिता की [पुण्य-वृद्धि] के लिये काकनादबोट-बिहार के चारों दिशाओं के आर्य संघ को अक्षय-नीवी के रूप में बारह दीनार दिया। इन दीनारों से प्राप्त होने वाले ब्याज से संघ में आये हुए एक भिक्षु को प्रतिदिन भोजन दिया जाय।
रत्न-गृह के लिये भी तीन दीनार दिया गया। इन तीन दीनारों के ब्याज से [रत्नगृह में] भगवान् बुद्ध के लिए नित्य तीन दीप जलाये जायँ। चर्तुर्बुद्ध (चार बुद्ध) के आसन के लिये भी एक दीनार दियाइसके ब्याज से चतुर्बुद्ध-आसन के बुद्ध के लिए नित्य दीप जलाया जाय।
स्वामिनी, सनसिद्ध-पत्नी, उपासिका, हरिस्वामिन् द्वारा प्रवर्तित चन्द्र-सूर्य के अस्तित्व काल तक बनी रहनेवाला [यह] अक्षय नीवी व्यवस्था इस शिलालेख [के रूप में] लिखी गयी। इति।
सम्वत् १३१ अश्वायुज दिन ५ ।
विश्लेषण
इस अभिलेख में किसी शासक के नाम का उल्लेख नहीं गया है। अंकित तिथि १३१ को गुप्त सम्वत् अनुमान कर इस लेख को फ्लीट ने कुमारगुप्त (प्रथम) अथवा उसके उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त के काल का अनुमान किया है। लिपि के आधार पर यह लेख निःसन्दिग्ध रूप से गुप्तकालीन है, तदनुसार इस पर अंकित तिथि भी गुप्त सम्वत् मानी जा सकती है।
विंसेंट स्मिथ ने डब्लू वास्ट के संग्रह में उपलब्ध कुमारगुप्त (प्रथम) के चाँदी के एक सिक्के पर वर्ष १३६ पढ़ा था। उनके कथन के इस आधार पर कुमारगुप्त (प्रथम) की अन्तिम तिथि १३६ समझी जाती रही है।
यह लेख हरिस्वामिनी नाम्नी बौद्ध-उपासिका द्वारा काकनादबोट (साँची) स्थित विहार हो अक्षय नीवि के रूप में दिये गये दान की घोषणा है। दान-दात्री का उल्लेख इस लेख में दो बार आरम्भ और अन्त में हुआ है। उसे उपासिका के अतिरिक्त स्वामिनी भी कहा गया है।
जे० एफ० फ्लीट ने इसे विहार-स्वामिनी का लघ्वीकरण माना है। साँची से ही उपलब्ध एक खण्डित स्तम्भ लेख में विहार-स्वामी और कुशीनगर स्थित बुद्ध की निर्वाण मूर्ति पर अंकित लेख में महाविहार-स्वामिन् विरुद अथवा उपाधि का प्रयोग हुआ है। फ्लीट ने इन दोनों को विहार के व्यवस्थापक की उपाधि माना है और महाविहार स्वामिन् को बड़ा और विहार स्वामिन को उसके अन्तर्गत छोटा अधिकारी अनुमान किया है।
डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त जी का मत है कि इन उपाधियों का सम्बन्ध वस्तुतः बौद्ध-विहार से हो तो भी इन दोनों ही उपाधियों का पारस्परिक कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों ही उपाधियों एक ही स्तर की हैं। एक का सम्बन्ध महाविहार से और दूसरे का सम्बन्ध सामान्य विहार से है।
प्रस्तुत लेख के प्रसंग में फ्लीट स्वामिनी को विहार-स्वामिनी का संक्षिप्तीकरण मानते हुए भी इसे धार्मिक संस्था से सम्बद्ध उपाधि नहीं मानते। वे इससे विहार-स्वामी की पत्नी का भाव ग्रहण करते हैं। परन्तु बौद्ध-विहार के सन्दर्भ में किसी व्यवस्थापक के गृहस्थ होने की कल्पना कुछ विचित्र और संदेहास्पद सी लगती है। विहार और महाविहार का व्यवस्थापक तो कोई गृह-त्यागी भिक्षु ही होता रहा होगा। परन्तु गृहस्थ का विहार व्यवस्थापक होना असम्भव भी नहीं माना जा सकता है।
बौद्ध संघ ने पुरुषों की तरह ही स्त्रियों को भी प्रव्रज्या लेने की छूट दे रखी थी। अतः निश्चित है कि भिक्षुओं की तरह ही भिक्षुणियाँ भी विहारों में रहती रही होंगी। उनकी व्यवस्था भिक्षु-विहारों से अलग होती रही होगी। उनके अपने विहार रहे होंगे। अतः उन विहारों की व्यवस्थापिका को ही विहार-स्वामिनी कहा जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान सत्य के निकट और स्वाभाविक होगा।
प्रस्तुत लेख के सन्दर्भ में द्रष्टव्य यह है कि स्वामिनी कही जानेवाली नारी का परिचय पत्नी के रूप में दिया गया है; भिक्षुणी होने के बाद तो पति-पत्नी जैसा सम्बन्ध रह ही नहीं जाता। दूसरी बात बौद्ध-संघ किसी भी भिक्षु-भिक्षुणी को अर्थ संचय की अनुमति नहीं देता। जब कोई भिक्षु या भिक्षुणी अर्थ-संचय कर ही नहीं सकता था, तो दान देने के लिये उसके पास धन कहाँ रहा होगा? स्पष्ट हैं कि इस लेख में स्वामिनी का प्रयोग विहार-स्वामिनी के भाव में नहीं, सीधे-सादे ढंग से गृह-स्वामिनी के भाव में हुआ है।
साँची प्रस्तर लेख के अनुसार जो धन दान दिया गया है, उसके मूल्य (मूल-धन) को अक्षुण्ण ( अक्षय ) रखने का विधान है, वह अक्षय नीवि है। उसके ब्याज का ही व्यय किया जा सकता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि काकनादबोट महाविहार उपासक उपासिकाओं की ओर से ट्रस्टी का कार्य भी करता और उनके धन से बैंक की तरह ब्याज के रूप में आय का साधन प्रस्तुत करता था। महाविहार दान-दाताओं से उपलब्ध पूँजी का उपयोग किस प्रकार करता था जिससे उसे व्यय के लिये ब्याज प्राप्त हो, अभी तक किसी सूत्र से नहीं जाना जा सका है। हो सकता है, श्रेणियों की तरह वह स्वयं ऋण देता और ब्याज प्राप्त करता रहा हो। अथवा वह स्वयं दान में प्राप्त पूँजी को किसी विश्वस्त श्रेणी में जमा कर ब्याज प्राप्त करता रहा हो।
साँची प्रस्तर लेख द्वारा दान दात्री ने तीन कार्यों को व्यवस्था की है —
(१) १२ दीनार के अक्षय-नीवि से प्राप्त ब्याज से नित्य एक भिक्षु के लिये भोजन।
(२) तीन दीनार के ब्याज से रत्न-गृह में नित्य तीन दीप का प्रज्वलन।
(३) एक दीनार के ब्याज से चतुर्बुद्धासन पर नित्य एक दीप का प्रज्वलन।
कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य :
- इसी तरह का उल्लेख साँची के एक अन्य लेख चन्द्रगुप्त द्वितीय का साँची अभिलेख में हुआ है।
- १२ दीनार की रकम से भिक्षु संघ को ब्याज के रूप में कितनी आय होती रही होगी, इसकी कोई उल्लेख नहीं है।
- दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के होते थे जिनका भार १४४ ग्रेन होता था। रूपक गुप्तकालीन चाँदी के सिक्के थे जिसका भार ३२.३६ ग्रेन होता था। दीनार और रूपक का १ : १६ अनुपात था।
- चतुर्बुद्धासन : एलेक्जेंडर कनिंघम ने चतुर्बुद्धासन से तात्पर्य स्तूप के चारों ओर लगी वेदिका के भीतर तोरणद्वारों के सामने बैठी बुद्ध-प्रतिमाओं से अनुमान किया है। कदाचित् फ्लीट की भी यही धारणा है। यदि दान-दात्री का यही अभिप्राय होता तो वह चार दिशाओं में स्थित चार बुद्ध-प्रतिमाओं के सम्मुख प्रज्वलन के लिए वह चार दीपों की व्यवस्था करती न कि केवल एक। अतः इसका तात्पर्य किसी शिलाफलक पर पंक्तिबद्ध बने बुद्ध की चार प्रतिमाओं से है। बुद्ध की ये चार प्रतिमाएँ चार भिन्न मुद्राओं – अभय, ध्यान, भूमि-स्पर्श और धर्म-चक्रप्रवर्तन मुद्रा की रही होंगी। यह भी हो सकता है कि वह शिला-फलक न होकर चार दिशाओं में चार भिन्न मुद्राओं की बुद्ध प्रतिमाओं से अंकित कोई मूर्ति-संयोजन रहा हो। ऐसी जैन प्रतिमाएँ प्रायः देखी जाती हैं।
कुमारगुप्त ( प्रथम ) का बिलसड़ स्तम्भलेख – गुप्त सम्वत् ९६ ( ४१५ ई० )
कुमारगुप्त प्रथम का उदयगिरि गुहाभिलेख (तृतीय), गुप्त सम्वत् १०६
मथुरा जैन-मूर्ति-लेख : गुप्त सम्वत् १०७ ( ४२६ ई० )
धनैदह ताम्रपत्र ( गुप्त सम्वत् ११३ )
तुमैन अभिलेख ( गुप्त सम्वत् ११६ )
मन्दसौर अभिलेख मालव सम्वत् ४९३ व ५२९
करमदण्डा शिवलिंग अभिलेख – गुप्त सम्वत् ११७ ( ४३६ – ३७ ई० )
दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख ( प्रथम ) गुप्त सम्वत् १२४ ( ४४३ – ४४ ई० )
दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख (द्वितीय) – गुप्त सम्वत् १२८ ( ४४७-४८ ई० )
मथुरा बुद्ध-मूर्ति लेख – गुप्त सम्वत् १२५ ( ४४४ ई० )