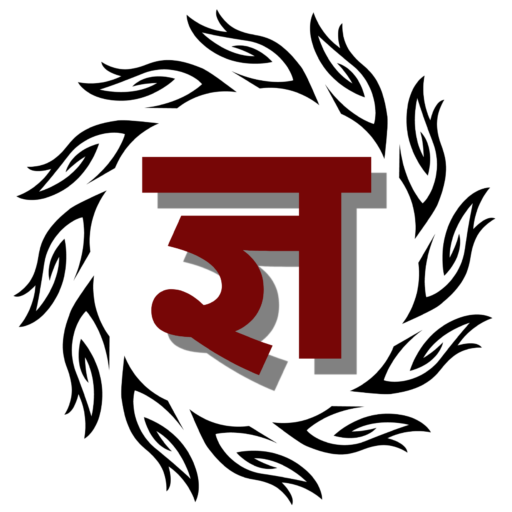भूमिका एटा (उत्तर प्रदेश) जिला अन्तर्गत अलीगंज तहसील से चार मील उत्तर-पश्चिम बिलसड़ पुवायाँ नामक एक ग्राम है। इस ग्राम के उत्तर-पश्चिमी कोने पर लाल पत्थर के बने चार टूटे स्तम्भ (दो गोल और दो चौकोर) खड़े हैं। इनमें से दोनों गोल स्तम्भों पर यह लेख समान रूप से अंकित है। एक पर वह १३ पंक्तियों में और दूसरे में १६ छोटी पंक्तियों में है। इसे १८७७-७८ ई० में एलेक्जेंडर कनिंघम ने ढूँढ निकाला था; १८८० ई० में उन्होंने इसका अनुवादसहित पाठ प्रकाशित किया। तदनन्तर फ्लीट ने उसे सम्पादित कर प्रकाशित किया। संक्षिप्त परिचय नाम :- कुमारगुप्त ( प्रथम ) का बिलसड़ स्तम्भलेख स्थान :- बिलसड़ पुवायाँ ग्राम, एटा जनपद; उत्तर प्रदेश भाषा :- संस्कृत लिपि :- परवर्ती ब्राह्मी समय :- गुप्त सम्वत् वर्ष ९६ अर्थात् ४१५ ई० ( ९६ + ३१९ ) विषय :- यह अभिलेख ध्रुवशर्मा नामक व्यक्ति द्वारा कार्तिकेय के मन्दिर में एक प्रवेश-द्वार तथा सत्र स्थापित करने की घोषणा है। इसमें गुप्त राजवंश की वंशावली मिलती है। मूलपाठ १. [ सिद्धम् ॥ ] [ सर्व्व-राजोच्छेत्तुः पृथिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदधि-सलिला-स्वा ] दित-यशसो २. [ धनद-वरुणेन्द्रान्तक-समस्य कृतान्त-परशोः न्यायागतानेक-गो-हि ] रण्य-कोटि-प्रदस्य चिरोत्सन्नाश्वमेधाहर्त्तुः ३. महाराज-श्रीगुप्त-प्रपौत्रस्स महाराज श्रीघटोत्कच-पौत्रस्य म [ हा ] राजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त पुत्रस्य ४. लिच्छ [ वि-दौहित्रस्य ] [ महादेव्यां कुमारदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजा ] धिराज श्री समुद्रगुप्त-पुत्रस्य ५. महादेव्यां दत्त [ देव्यामुत्पन्नस्य स्वयमप्रतिरथस्य परम भागवत ] स्य महाराजाधिराज-श्री चन्द्रगुप्त-पुत्रस्य। ६. महादेव्यां ध्रुवदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज-श्रीकुमारगुप्तस्याभि [ व ] – द्र्धमान-विजय-राज्य-संवत्सरे षणवते ७. [ अस्यान्दि ] वस पूर्व्वायां भगवतस्त्रैलोक्य-तेजस्संभार सं [ भृ ] ताद्भूत-मूर्त्ते-र्ब्रह्मण्यदेवस्य ८. ….. निवासिनः स्वामि-महासेनस्यायतने [ ऽ ] स्मिन्कार्त्त-युगाचार-सद्धर्म्म-वर्त्मानुयायिना। ९. [ माता ] ……. [ प ] र्षदा मानितेन ध्रुवशर्म्मणा कर्म्म महत्कृतेदम्। १०. कृ [ त्व ] [ नेत्र ] भिरामां मु [ नि-वसति मिह स्व ] र्ग्ग-सोपान [ रू ] पां [ । ] कौबेरच्छन्दबिम्बां स्फटिकमणिदलाभास गौरां प्रतो [ लि ] म्। ११. प्रासादा [ ग्राभि ] रूपं गुणवर-भवनं [ धर्म्म-स ] यथावत्। पुण्येष्वेवाभिरामं व्रजति शुभमतिस्ताद शर्मा ध्रुवो ( ऽ ) स्तु॥ १२. ……..स्य ….. शुभामृतवर-प्रख्यात-लब्धा भुवि। भक्ति-हीन-सत्व-समता कस्तं न संपूजयेत्। १३. येनापूर्व्व-विभूति-सञ्चय-चयैः …….. – …….. – । तेनायं ध्रुवशर्म्मणा स्थिर-वरस्तभो [ च्छ्र ] यः कारतिः। हिन्दी अनुवाद सिद्धि हो। सब राजाओं के उन्मूलक पृथिवी पर अप्रतिरथ ( जिसके समान पृथिवी पर अन्य कोई न हो ), चारों समुद्र के जल से आस्वादित कीर्तिवाले, कुबेर ( धनद ), वरुण, इन्द्र तथा यम (अन्तक) के समान, कृतान्त के परशु-तुल्य, न्याय से उपलब्ध अनेक गौ तथा कोटि हिरण्य ( सिक्के ) के दानदाता, चिरोत्सन्न-अश्वमेधहर्ता महाराज श्रीगुप्त के प्रपौत्र, महाराज श्री घटोत्कचगुप्त के पौत्र, महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त के पुत्र, लिच्छवि-दौहित्र महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त के महादेवी दत्तदेवी से उत्पन्न, अप्रतिरथ, परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त के महादेवी ध्रुवदेवी से उत्पन्न पुत्र महाराज श्री कुमारगुप्त के वर्तमान विजय राज्य का संवत्सर छियानवे ……… निवासी ( स्थित ) स्वामीमहासेन के, जो त्र्यलोक्य के तेज से आवृत भगवान ब्रह्मण्यदेव हैं, इस आयतन ( मन्दिर ) में, कृतयुग ( सत्ययुग ) के आचार के अनुसार जो सद्धर्म वर्तमान है, उसका पालन करनेवाले तथा …… परिषद् में आदर प्राप्त करनेवाले ध्रुवशर्मा द्वारा स्वर्ग के सोपानस्वरूप नयनाभिराम, मुनियों का निवास-स्थान, तथा कुबेरच्छन्द [ नामक मणि ] के समान स्फटिक मणि-मालाओं की प्रभा से आच्छादित प्रतोली ( प्रवेश-द्वार ) तथा अग्र-प्रासाद के रूप में गुणवर-भवन, धर्म-सत्र का निर्माण किया गया। इसके पुण्य के स्वरूप [ दीर्घ काल तक ] मनोहारी रूप से ध्रुवशर्मा विचरण करता रहे। ……. इस पृथ्वी पर जिसकी शुभ और अमर ख्याति ……. [ शायद ही कोई ऐसा ] भक्ति रहित हो जो सत्व और समभाव से इसकी पूजा न करता हो। इस पूर्वकथित [ वास्तु ] का [ निर्माण कराकर ] विभूति का संचय ….. उस ध्रुवशर्मा ने दृढ़ स्तभ…….. टिप्पणी यह अभिलेख ध्रुवशर्मा नामक व्यक्ति द्वारा महासेन ( कार्तिकेय ) के मन्दिर में एक प्रतोली ( प्रवेश-द्वार ) तथा सत्र स्थापित करने की घोषणा है। इस अभिलेख का ऐतिहासिक महत्त्व केवल इतना ही है कि इसमें गुप्तवंश के परिचय की अभिव्यक्ति करनेवाले वंशावली का वह प्रारूप प्राप्त होता है जो आगे रूढ़ होकर गुप्त शासकों की मुद्राओं एवं आलेखों में प्रयोग होता रहा। इस वंश-परिचय में समुद्रगुप्त के लिये प्रायः उन्हीं विरुदों का प्रयोग हुआ है जिनका प्रयोग हरिषेण ने प्रयाग-प्रशस्ति में किया है। उन विरुदों के अतिरिक्त दो विरुद नये हैं, जो हमारा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। वे हैं —— सर्व-राजोच्छेता और चिरोत्सन्न-अश्वमेध-हर्तुः। सर्वराजोच्छेता ( सभी राजाओं का उन्मूलन करनेवाला ) विरुद का प्रयोग सर्वप्रथम हमें काचगुप्त के सिक्कों पर देखने को मिलता है; इस कारण अनेक विद्वानों—विसेंट स्मिथ, फ्लीट, एलन आदि ने काचगुप्त के सिक्कों को समुद्रगुप्त का सिक्का बताने का प्रयास किया है और कहा है कि काच उसका अपर नाम था। इस प्रसंग में द्रष्टव्य यह है कि हरिषेण ने प्रयाग प्रशस्ति में इस प्रकार के किसी विरुद का प्रयोग न कर उसे अनेक-भ्रष्ट-राजोत्सन्न राजवंश प्रतिष्ठापक कहा है, जो इस विरुद के भाव के सर्वथा विपरीत है। इसलिए इस विरुद का प्रयोग समुद्रगुप्त ने अपने लिये कभी न किया होगा। इसका प्रयोग निःसन्देह उसके जीवन-काल के बाद ही आरम्भ हुआ होगा। इस प्रसंग में यह भी द्रष्टव्य है कि इस विरुद का प्रयोग समुद्रगुप्त तक ही सीमित नहीं है प्रभावतीगुप्ता के पूना-ताम्र-शासन में चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) को भी सर्वराजोच्छेता कहा गया है | चिरोत्सन्न अश्वमेध-हर्तुः का अर्थ फ्लीट ने — ‘दीर्घकाल से बन्द अश्वमेध ( यज्ञ ) को पुनर्प्रचलित करनेवाला ( one who has restored the Ashvamedha, that had been long in abeyance ) किया है। इनके इस अनुवाद को सभी विद्वान् अन्धानुकरण कर, स्वीकार करते चले आ रहे हैं। किन्तु समुद्रगुप्त से पूर्व अनेक राजाओं — शुंगवंशी पुष्यमित्र, कलिंग नरेश खारवेल, सातवाहन वंशी सातकर्णि, वाकाटक-वंशी प्रवरसेन एवं भारशिव ने अश्वमेध यज्ञ किये थे। कुछ ने तो समुद्रगुप्त से कुछ ही काल पूर्व किया था इस अनुवाद को ठीक मानें तो समुद्रगुप्त के लिये प्रयुक्त यह विरुद सत्य के सर्वथा विपरीत ठहरता है किन्तु इस विरुद को मात्र अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः फ्लीट एवं अन्य विद्वानों ने इसे समझने की समुचित चेष्टा नहीं की है। चिरोत्सन्न शब्द का प्रयोग अश्वमेध के प्रसंग में ही शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। उसमें इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि ‘यज्ञ के अनेक कर्म तत्त्व भूले जा चुके हैं अतः इसके परिहारस्वरूप यज्ञ-कर्ता के लिये आवश्यक है