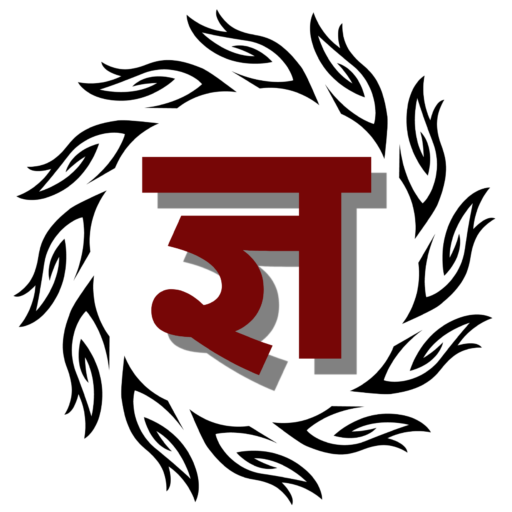स्कंदगुप्त का भीतरी स्तम्भलेख
भूमिका स्कंदगुप्त का भितरी स्तम्भलेख या भीतरी स्तम्भलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत सैदपुर से पाँच मील उत्तर-पूर्व स्थित भितरी नामक ग्राम में खड़े लाल पत्थर के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। यह स्तम्भ सम्भवतः उस मन्दिर के आगे लगा ध्वज था जिसके छेंकन आदि के कुछ भाग काशी विश्वविद्यालय द्वारा कराये गये उत्खनन में कुछ वर्ष पूर्व प्रकाश में आये हैं। १८३४ ई० में ट्रेगियर महोदय ने सर्वप्रथम देखा था। उस समय अभिलेखवाला अंश मिट्टी के नीचे दबा था। एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जब उसके चारों ओर की मिट्टी हटायी गयी, तो यह लेख प्रकाश में आया। १८३६ ई० में उन्होंने इसके प्राप्त होने की सूचना प्रकाशित की। १८६७ ई० में रेवरेण्ड डब्लू एच० मिल ने इसे अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया। १८७१ ई० में कनिंघम ने, १८७५ ई० में भाऊ दाजी ने और १८८५ ई० में भगवानलाल इन्द्रजी ने अपने-अपने पाठ और अनुवाद प्रकाशित किये। तदुपरांत जे० एफ० फ्लीट ने उसे सम्पादित कर Corpus Inscriptionum Indicarum में प्रकाशित किया। बाद में भण्डारकर ने उसका पुनर्परीक्षण किया है। संक्षिप्त परिचय नाम :- स्कंदगुप्त का भीतरी स्तम्भलेख या भितरी स्तम्भलेख [ Bhitari Stone Pillar of Skandgupta ] स्थान :- गाजीपुर जनपद; उत्तर प्रदेश भाषा :- संस्कृत लिपि :- उत्तरी ब्राह्मी समय :- गुप्त सम्वत् १४८ ( ४६७ ई० ), स्कंदगुप्त का शासनकाल विषय :- स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का विवरण मूलपाठ १. [सिद्धम् ॥] [सर्व]रा[जो]च्छेतुः पृथिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदधिसलिला-स्वादित-यशसो धनद-वरुणेन्द्रान्तक-स[मस्य] २. कृतान्त-परशोः न्यायागतानेक-गो-हिरण्य [को]टि-प्रदस्य चिरोत्सन्नाश्वमेधाहर्त्तुर्महाराज श्रीगुप्तप्रपौत्र [स्य] ३. महाराज-श्रीघटोत्कचपौत्रस्य महाराजाधिराज-श्रीचन्द्रगुप्त-पुत्रस्य लिच्छवि-दौहित्रस्य महादेव्यां कुमार-देव्या- ४. मुत्पन्नस्य महाराजाधिराज-श्रीसमुद्रगुप्तस्य पुत्रस्तत्परिगृहीतो महादेव्यान्दत्तदेव्यामुत्पन्नः स्वयं चाप्रतिरथः ५. परम-भागवतो-महाराजाधिराज-श्रीचन्द्रगुप्तस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुद्धयातो महादेव्यां ध्रुवदेव्यामुत्पन्नः परम- ६. [भा]गवतो महाराजाधिरा[ज]-श्रीकुमारगुप्तस्तस्य[।] प्रथित-पृथुमति-प्रभाव-शक्तेः पृथु-यशसः पृथिवी-पतेः पृथुश्रीः [।] ७. पि[तृ]-प-[रि]-गत-पादपद्म-वर्ती प्रथित-यशाः [पृ]थिवीपतिः सुतोऽयम् [॥ १] [ज]गति भु[ज]-बलाढ्यो गुप्त वंशै[क]वीरः प्रथित-विपुल- ८. नामा नामतः स्कन्दगुप्तः [।] सुचरित-चरितानां येन वृत्तेन-वृत्तं न विहितमथात्मा तान-[धीदा?]-विनतिः [॥ २] विनय- ९. बल-सुनीतैर्व्विक्क्रमेण-क्क्रमेण प्रतिदिनमभियोगादीप्सितं ये[न]ल[ब्ध्वा] [।] स्वभिमत-विजिगीषा-प्रोद्यतानां परेषां प्रणि-हित इव ले[भे सं]विधानोपदेशः [II ३] १०. विचलित-कुल-लक्ष्मी-स्तम्भनायोद्यतेन क्षितितल-शयनीये येन नीता त्रियामा [।] समु- ११. दित ब[ल]कोशन्-राष्ट्र-मित्राणियक्त्वा क्षितिप-चरण-पीठे स्थापितो वाम-पादः [॥ ४] प्रसभमनुपमर्द्रिर्धस्त-शस्त्र-प्रतापैर्विन[य] [स]मु [चितैश्च] क्षान्ति-शौयैर्न्निरूढम् [।] १२. चरितममलकीर्त्तेर्गीयते यस्य शुभ्रं दिशि दिशि परितुष्टैराकुमारं मनुष्यैः [॥ ५] पितरि दिवमुपेते १३. विप्लुतां वंश-लक्ष्मीं भुज-बल-विजितारिर्य्यः प्रतिष्ठा[प्य भूयः] [।] जितमिति परितोषान्मातरं सास्र नेत्रां हतिरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्यु[पे- १४. [तः] [॥ ६] [स्वै]र्द्द[ण्डैः] [द्विषदो व्यापेत्य] चलितं वंशं प्रतिष्ठाप्य यो बाहुभ्यामवनिं विजित्य हि जितेष्वार्त्तेषु कृत्वा दयाम् [।] नोत्सिक्तो [न] च विस्मितः प्रतिदिनं १५. [संवर्द्धमान]-द्युति-गतिश्च स्तुतिभिश्च-वृत्तकथनं यं [प्र]णयत्यार्तं [॥ ७ ] हूणैर्य्यस्य समागतस्य समरे दोर्भ्यां धरा कम्पिता भीमावर्त्त-करस्य १६. शत्रुषु शरा[विनयस्य दुर्घर्षिनः] [।] …………….. लिखितं प्रख्यापितो [दीप्तिनद्यो नभी तै लक्ष्यत इव श्रोत्रेषु सारङ्ग ध्वनिः [॥ ८] १७. [स्व] पितुः कीर्त्ति — — — — …… — …… [।] — — — — [मुक्तिभिर्युक्त] — — — — …… — …… — [॥ ९] [प्रकार्य्या] प्रतिमाका चिठप्रतिमां तस्य शाङ्गिणः [।] १८. [सु]प्रतीतश्चकारेमां या [वदाचन्द्र-तारकम्] [॥ १०] इह-चैनं प्रतिष्ठाप्य सुप्रतिष्ठित-शासनः [।] ग्राममेनं स विद[धे] पितुः पुण्याभिवृद्धये [॥ ११] १९. अतो भगवतो मूर्त्तिरियं यश्चात्र संस्थितः (?) [।] उभयं निर्द्दिदेशासौ पितुः पुण्याय-पुण्य-धीरिति [॥ १२] हिन्दी अनुवाद सिद्धि हो! सब राजाओं के उन्मूलक; पृथ्वी पर अप्रतिरथ (जिसके समान पृथ्वी पर अन्य कोई न हो); चारों समुद्र के जल से आस्वादित कीर्तिवाले; कुबेर (धनद), वरुण, इन्द्र तथा यम (अन्तर) के समान; कृतान्त के परशु-तुल्य; न्याय से उपलब्ध अनेक गो तथा कोटि हिरण्य (सिक्के) के दान-दाता; चिरोत्सन्न-अश्वमेध हर्त्ता; महाराज श्रीगुप्त के प्रपौत्र; महाराज घटोत्कचगुप्त के पौत्र; महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त के पुत्र; लिच्छवि-दौहित्र, महादेवी कुमारदेवी [के गर्भ से उत्पन्न] महाराज समुद्रगुप्त उनके पुत्र, उनके परिगृहीत, महादेवी दत्तदेवी [के गर्भ से उत्पन्न] स्वयं भी अप्रतिरथ; परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त उनके पुत्र तथा पादानुगामी महादेवी ध्रुवदेवी से उत्पन्न परमभागवत महाराजाधिराज कुमारगुप्त — [१-६] वे प्रबल मेधा से सत्पन्न (प्रथित पृथु-मति), शक्तिसम्पन्न (प्रभाव-शक्तेः) महान् यशस्वी (पृथु-यशस), विख्यात (पृथु-श्री) थे; [उन्हीं] पिता के चरण-कमल पर भ्रमर की भाँति मँडरानेवाला, शासक ( पृथ्वी-पति), यह पुत्र है। जगत् में अपनी भुजाओं के लिये प्रख्यात, गुप्त वंश के इस वीर का नाम स्कन्दगुप्त है। [६-८] उसका चरित्र ही सुचरित है, उसकी धर्म-परायणता कथनीय (वृत) है; वह प्रशस्तमार्गगामी (धर्मविहित) है; [वह] निर्मल आत्मा और विनीत हैं। विनय, बल, विक्रम उसने दाय (क्रम) में प्राप्त किया है लोक व्यवहार का ध्यान रखते हुए [उसने] विजय की दृढ़ इच्छा रखनेवाले शत्रुओं को भी पराभूत करने की कला में दक्षता प्राप्त की है। [६-१०] अपने कुल की विचलित लक्ष्मी को पुनः स्थापित करने के प्रयास में उसे सारी रात पृथ्वीरूपी शैया पर बितानी पड़ी। [अन्ततोगत्वा] बल, कोष, राष्ट्र (प्रजा) और मित्रों की सहायता से अपने शत्रुओं को अपने चरणों का आसन बनाने (अर्थात् कुचलने) में सफल रहा। उसने अपने शस्त्रों के अतुल प्रताप से अपने शत्रुओं का विनाश कर दिया। उस अमल कीर्तिवाले राजा का शुभ चरित अपने समुचित विनय, शान्ति एवं शौर्य आदि के कारण दूर-दूर तक फैला हुआ है। चारों ओर बालक वृद्ध सभी प्रसन्न भाव से उसका गुणगान करते रहते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात् उसने वंश की विलुप्त लक्ष्मी को अपने बाहु-बल द्वारा शत्रुओं को विजित कर फिर से स्थापित किया। और तब वह विजयी होकर अपनी आँसू भरे माँ के पास परितोष के निमित्त उसी प्रकार गया जिस प्रकार कृष्ण देवकी के पास गये थे। उसने अपनी सेना की सहायता से वंश की विचलित प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। अपने बाहुबल से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। साथ ही, उसने विजित एवं आर्तजनों के प्रति दया भाव भी व्यक्त किया। अपने दिनों-दिन बढ़ते हुए प्रताप के प्रति उसने कभी न तो गर्व किया और न कभी आश्चर्य प्रकट किया। [वरन्] वृत्त कथन कहने वाले ही उसे अपने गीतों और स्तुतियों में उसे आर्य कहा करते थे। युद्ध में उसके बाण शत्रुओं में हलचल (जलावर्त) मचा देते थे और आकाश और नदी के बीच धनुष के टंकार प्रतिध्वनित हो उठते थे, और जब हूण अपने दोनों बाहुओं के सहारे पृथ्वी पर गिरते थे तो पृथ्वी कम्पित हो उठती थी। अपने पिता की कीर्ति …….. किसी की प्रतिमा बनाना कर्त्तव्य है, यह सोचकर जब तक चाँद और तारे रहें तब तक स्थायी रहने के निमित्त (उसने शार्ङ्गिण की प्रतिमा [यहाँ] प्रतिष्ठापित की और [अपने] पिता की पुण्य की वृद्धि के लिये उसने इस ग्राम को (उस देवता) को प्रदान किया; उसीका यह सुप्रतिष्ठित शासन है। इस प्रकार भगवान् की यह प्रतिमा तथा जहाँ वह स्थापित है [ वह गाँव], दोनों उसने पुण्य अर्जन के निमित्त अर्पित किया। टिप्पणी
स्कंदगुप्त का भीतरी स्तम्भलेख Read More »