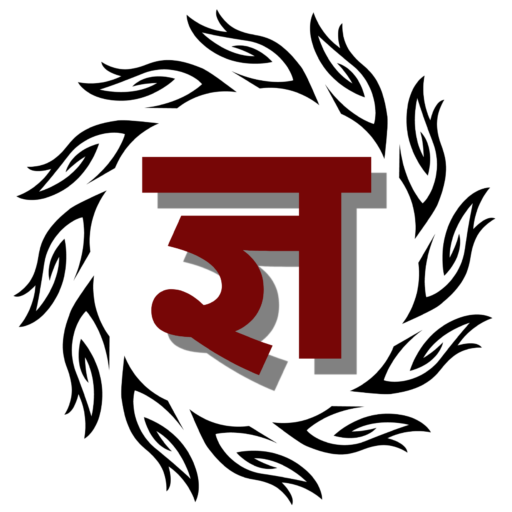अशोक का सातवाँ स्तम्भलेख
भूमिका सप्तस्तम्भ लेखों में से सातवाँ स्तम्भलेख अशोक के अन्य स्तम्भलेखों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह मात्र दिल्ली-टोपरा स्तम्भ पर ही अंकित है। दिल्ली-टोपरा पर खुदे लेख अन्यत्र छः स्थानों से मिले स्तम्भलेखों में सबसे प्रसिद्ध स्तम्भ लेख है। यही एकमात्र ऐसा स्तम्भ हैं जिसपर सातों लेखों का एक साथ अंकन मिलता है। शेष पाँच पर मात्र छः लेख ही प्राप्त होते हैं। मध्यकाल के प्रसिद्ध इतिहासकार शम्स-ए-शिराज़ के अनुसार यह स्तम्भ मूलतः टोपरा में था। इसे दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने वहाँ से लाकर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित करवा दिया था। तबसे इसको दिल्ली-टोपरा स्तम्भलेख के नाम से जाना जाने लगा। इस स्तम्भ के कुछ अन्य नाम भी हैं; यथा – भीमसेन की लाट, दिल्ली-शिवालिक लाट, सुनहरी लाट, फिरोजशाह की लाट आदि। सातवाँ स्तम्भलेख : संक्षिप्त परिचय नाम – अशोक का सातवाँ स्तम्भलेख या सप्तम स्तम्भलेख ( Ashoka’s Seventh Pillar-Edict ) स्थान – दिल्ली-टोपरा संस्करण। यह मूलतः टोपरा, हरियाणा के अम्बाला जनपद में स्थापित था, जिसको दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुग़लक़ ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित करवा दिया था। तभी से इसको दिल्ली-टोपरा स्तम्भ कहा जाने लगा। भाषा – प्राकृत लिपि – ब्राह्मी समय – मौर्यकाल, अशोक के राज्याभिषेक के २६ वर्ष बाद अर्थात् २७वें वर्ष। विषय – इस स्तम्भलेख में अशोक के विविध लोककल्याणकारी कार्यों की सूची मिलती है। यह अशोक के स्तम्भ लेखों में से सबसे बड़ा स्तम्भलेख है। सातवाँ स्तम्भलेख : मूलपाठ [ दिल्ली-टोपरा संस्करण ] १ – देवानंपिये पियदसि लाजा हेवं आहा [ । ] ये अतिकन्तं २ – अन्तलं लाजाने हुसु हेवं इछिसु कथं जने ३ – धम्म-वढिया वढेया [ । ] नो चु जने अनुलुपाया धम्म-वढिया ४ – वढिया [ । ] एतं देवानंपिये पियदसि लाजा हेवं आहा [ । ] एस मे ५ – हुथा [ । ] अतिकन्तं च अन्तंलं हेवं इछिसु लाजाने कथं जने ६ – अनुलुपाया धम्म-वढिया वढेया ति [ । ] नो च जने अनुलुपाया ७ – धम्म – वढिया वढिया [ । ] से किनसु जने अनुपटिपजेया [ । ] ८ – किनसु जने अनुलुपाया धम्म-वढिया वढेया ति [ । ] किनसु कानि ९ – अभ्युंनामहेयं धम्म वढिया ति [ । ] एतं देवानंपिये पियदसि लाजा हेवं १० – आहा [ । ] में हुथा [ । ] धम्म-सावनानि सावापयामि धम्मानुसथिनि ११ – अनुसासामि [ । ] एतं जने सुतु अनुपटीपजीसति अभ्युंनमिसति १२ – धम्म-वढिया च वाढं वढिसति [ । ] एताये मे पठाये धम्म-सावनानि सावापितानि धम्मानुसथिनि विविधानि आनपितानि य [ था ] [ । ] मा पि बहुने जनसि आयता ए ते पलियोवदिसन्ति पि पविथलिसन्ति पि [ । ] लजूका पि बहुकेसु पान-सत-सहसेसु आयता [ । ] ते पि मे आनपिता हेवं च पलियोवदाथ १३ – जनं धम्म-युतं [ । ] देवानंपिये पियदसि हेवं आहा [ । ] एतमेव मे अनुवेखमाने धम्म-थम्भानि कटानि धम्म-महामाता कटा धम्म [ सावने ] कटे [ । ] देवानंपिये पियदसि लाजा हेवं आहा [ । ] मगेसु पि मे निगोहानि लोपापितानि छायोपगानि होसन्ति पसुमुनिसानं अम्बा-वडिक्या लोपापिता [ । ] अढकोसिक्यानि पि मे उदुपानानि १४ – खानापापितानि निंसिढया च कालापिता [ । ] आपानानि में बहुकानि तत तत कालापितानि पटी भोगाये पसु मुनिसानं [ । ] ल [ हुके ] [ सु ] एक पटीभोगे नाम [ । ] विविधाया हि सुखायनाया पुलिमेहि पि लाजीहि ममया च सुखयिते लोके [ । ] इमं चु धम्मानुपटीपती अनुपटीपजन्तु ति एकदथा मे १५ – एस कटे [ । ] देवानंपिये पियदसि हेवं आहा [ । ] धम्म-महामाता पि मे ते बहुविधेसु अठेसु आनुगहिकेसु वियापटासे पवजीतानं चेव गिहिथानं चन [ च ] सव- [ पांस ] डेसु पि च वियापटासे [ । ] संघठसि पि मे कटे इमे वियापटा होहन्ति ति हेमेव बाभनेस आजीविकेसु पि मे कटे १६ – इमे वियापटा होहन्ति ति निगंठेसु पि मे कटे इमे वियापटा होहन्ति नाना-पासण्डेसु पि मे कटे इमे वियापटा होहन्ति ति पटिविसिठं पटीविसिठं तेसु तेसु ते ते [ महा ] माता [ । ] धम्म-महामाता चु मे एतेसु चेव वियापटा सवेसु च अन्नेसु पासण्डेसु [ । ] देवानं पिये पियदसि लाजा हेवं आहा [ । ] १७ – एते च अन्ने च बहुका मुखा दानविसगसि वियापटासे मम चेव देविनं च [ । ] सवसि च मे ओलोधनसि ते बहुविधेन आकालेन तानि तानि तुठायतनानि पटी [ — ] [ दयन्ति ] हिद चेव दिसासु च [ । ] दालकानां पि च मे कटे अन्नानं च देवि-कुमालानं इमे दानविसगेसु वियापटा होहन्ति ति १८ – धम्मापदानठाये धम्मानुपटिपतिये [ । ] एस हि धम्मापदाने धम्मपटीपति च या इयं दया दाने सचे सोचवे मदवे साधवे च लोकस हेवं वढिसति ति [ । ] देवानंपिये [ पियदसि ] लाजा हेवं आहा [ । ] यानि हि कानिचि ममिया साधवानि कटानि तं लोके अनूपटीपन्ने तं च अनुविधियन्ति [ । ] तेन वढिता च १९ – वढिसन्ति च मातापितिसु सुसुसाया गुलुसु वयो-महालकानं अनुपटीपतिया बाभन-समनेसु कपन-वलाकेसु आव दास-भटकेसु सम्पटीपतिया [ । ] देवानंपिये पियदसि लाजा हेवं आहा [ । ] मुनिसानं चु या इयं धम्मवढि वढिता दुवेहि येव आकालेहि धम्म नियमेन च निझतिया च [ । ] २० – तत चु लहु से धम्म-नियमे निझतिया व भुये [ । ] धम्म नियमे चु खो एस ये मे इयं कटे इमानि च इमानि जातानि अवधियानि [ । ] अन्नानि पि चु बहुकानि धम्म-नियमानि यानि से कटानि [ । ] निझतिया व चु भुये मुनिसानं धम्म-वढि वढिता अविहिंसाये भूतानं २१ – अनालम्भाये पानान [ । ] से एताये अथाये इयं कटे पुता-पपोति के चन्दम-सुलियिके होतु ति तथा च अनुपटीपजन्तु ति [ । ] हेवं हि अनुपटीपजन्तं हिदत-पालते आलधे होति [ । ] सतविसति-वसाभिसितेन मे इयं धम्मलिपि लिखापापिता ति [ । ] एतं देवानंपिये आहा [ । ] इयं २२ – धम्मलिपि अत अथि सिला-थम्भानि वा सिला-फलकानि वा तत कटविया एन एस चिलठितिके सिया [ । ] संस्कृत छाया देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा एवमाह। वदतिक्रान्तमन्तरं राजानोऽभवन्तेवमैच्छन् कथं जनं धर्मवद्धिर्वर्धनीया। न तु जनेऽनुरूपया धर्मवद्धिर्वधिता। अत्र देवानां प्रियः प्रियदर्शी राजा एवमाह। एतन्ते भूतम्। अतिक्रान्तमनरमेवैमैच्छन् राजनः कथं जनेऽनुरूपा धर्मवद्धिर्वर्धनीयेति। न च जनेऽनुरूपा धर्मवद्धिर्वधिता। तत्केनस्थित् जनोऽनुप्रतिपद्यते केनस्थित् जनेऽनुरूपा धर्मवद्धिर्वर्धनीयेति। केनस्थि केषामभ्युमन्नमयेहं धर्मवद्धिमिति। अत्र देवानां प्रियः प्रियदर्शी राजैवमाह। एतन्मे भूतम्। धर्मश्रावणानि, श्रावयामि, धर्मानुशिष्टीरनुशास्मि। एतानि जन, श्रुत्वा अनुप्रतियत्स्यते, अभ्पुन्नस्यति धर्मवद्धिश्च वाढं वर्धिष्यते। एतस्मै मया अर्थाय धर्मश्रावणानि श्रावितानि धर्मानुशिष्टयो विविधा आज्ञापिताः। यथा मे पुरुषा अपि बहुषु जनेष्वायत्ताः, एते परितो वदिष्यन्त्यपि प्रविस्तारयिष्यन्तपि। रज्जुका
अशोक का सातवाँ स्तम्भलेख Read More »