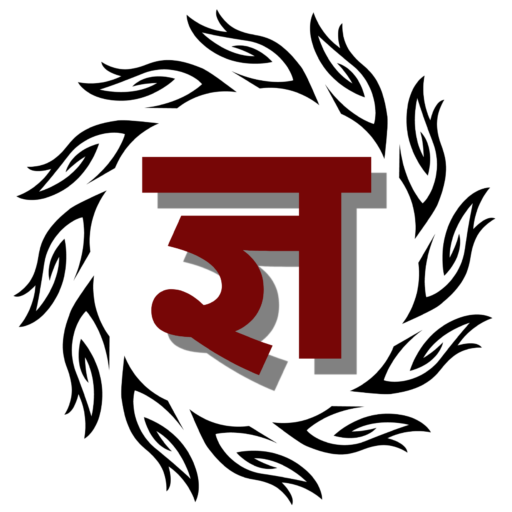अशोक का तीसरा स्तम्भलेख
भूमिका सप्तस्तम्भ लेखों में से तीसरा स्तम्भलेख अशोक द्वारा पाप क्या है? इसको बताया गया है। साथ ही आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। दिल्ली-टोपरा स्तम्भलेख सबसे प्रसिद्ध स्तम्भ लेख है। इसकी प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि केवल इसी पर अशोक के सातों लेख अंकित है जबकि अन्य स्तम्भों पर छः लेख ही प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन इतिहासकार शम्स-ए-शिराज़ के अनुसार टोपरा से इसको फिरोजशाह तुगलक ने लाकर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित संस्थापित करवाया था। इसी कारण इसको दिल्ली-टोपरा स्तम्भ कहा जाता है। इस स्तम्भ के कुछ अन्य नाम भी हैं; जैसे – भीमसेन की लाट, दिल्ली-शिवालिक लाट, सुनहरी लाट, फिरोजशाह की लाट आदि। तीसरा स्तम्भलेख : संक्षिप्त परिचय नाम – अशोक का तीसरा स्तम्भलेख या तृतीय स्तम्भलेख ( Ashoka’s Third Pillar-Edict ) स्थान – दिल्ली-टोपरा संस्करण। यह मूलतः टोपरा, हरियाणा के अम्बाला जनपद में स्थापित था, जिसको दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुग़लक़ ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित करवा दिया था। इसीलिए इसको दिल्ली-टोपरा स्तम्भ भी कहते है। भाषा – प्राकृत लिपि – ब्राह्मी समय – मौर्यकाल विषय – कौन-कौन से पाप हैं, इसकी व्याख्या। आत्मनिरीक्षण करने का सुझाव। तीसरा स्तम्भलेख : मूलपाठ १ – देवानं पिये पियदसि लाज हेवं अहा [ । ] कयानंमेव देखति इयं २ – कयाने कटे ति [ । ] नो मिन१ पापं देखति इयं मे पापे कटे ति इयं वा आसिनवे ३ – नामा ति [ । ] दुपटिवेखे चु खो एसा [ । ] हे चु खो एस देखिये [ । ] इमानि ४ – आसिनव-गामिनि नाम अथ चंडिये निठूळिये ( निठूलिये ) कोधे माने इस्या ५ – कालनेन व हकं मा पळिभसयिसं ( पलिभसयिसं ) [ । ] एस ( एक ) वाढ़ देखिये [ । ] इयं में ६ – हिदतिकाये इयंमन मे पाळतिकाये ( पालतिकाये ) [ ॥ ] १मेरठ संस्करण में ‘मिना’ पाठ मिलता है। संस्कृत छाया देवानां प्रियः प्रियदर्शी राजा एवं आह। कल्याणं एवं पश्यति इदं मया कल्याणं कृतं इति। नो मनाक पापं कृतं इति इदं वा आसिनवं नाम इति। दुष्प्रत्यवेक्ष्यं तु खलु एतत्। एवं तु खलु एतत् पश्येत् इमानि आसिनवगामीनि नाम यथा चाण्ड्यं, नैठुर्य, क्रोधः, मानः, ईर्ष्या कारणेन एवं अहं मा परिभ्रंशयिष्यामि। सतत् वाढं पश्येत् इदं मे एहिकाय इद अन्यत् मे पारत्रिकाय। हिन्दी अनुवाद १ – देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा – मनुष्य कल्याण ही देखता है। मैंने यह २ – कल्याण किया। वह थोड़ा भी पाप नहीं देखता कि यह पाप मैंने किया या यह पाप है। ३ – यह सचमुच कठिनाई से देखा जा सकता है पर इसे अवश्य देखना चाहिए कि यह ४ – पाप की ओर ले जाते है — चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या ५ – इनके कारण मैं अपने को भ्रष्ट कर दूँ इसे गम्भीरता से देखना चाहिए कि ये ६ – मेरे इस लोक के लाभ के लिए हैं और ये परलोक के कल्याण के लिए है। टिप्पणी इस स्तम्भलेख ( दूसरा स्तम्भलेख ) में अशोक ने अत्मनिरीक्षण करने को कहा है। आगे वे इसका कारण यह बताते हैं कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को तो देखता है परन्तु कुकृत्यों की अवहेलना कर देता है। इसीलिए उसको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि वस्तुतः कृत कर्मों का को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि अमुक कर्म लौकिक और पारलौकिक दृष्टि से अच्छा है अथवा नहीं। जिस प्रकार दूसरे स्तम्भलेख में अशोक ने धर्मिक कृत्यों को गिनाया है ठीक उसी तरह अकरणीय पाप कर्मों को भी यहाँ वर्णित किया है; यथा – चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या। पहला स्तम्भलेख दूसरा स्तम्भलेख
अशोक का तीसरा स्तम्भलेख Read More »