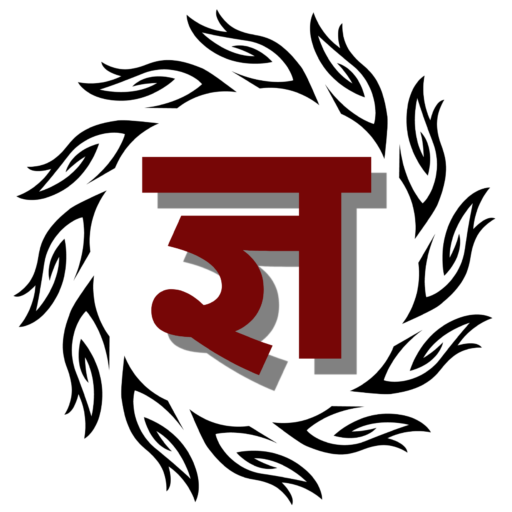भूमिका मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के के मथुरा जनपद से मिला है जोकि वर्तमान में लंदन के ब्रिट्रिश संग्रहालय में रखा गया है। यह सिंह स्तम्भ लाल बलुआ पत्थर ( Red Sandstone ) का बना है। यह अभिलेख अव्यवस्थित ढंग लिखा हुआ है जिससे कि इसका उद्वाचन कठिनाई उत्पन्न करता है। अभिलेख-विशारदों ने उसे खंडों में बाँटकर पढ़ने और फिर इन खंडों का तारतम्य बिठाकर व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने करने का प्रयास किया है। मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख : संक्षिप्त परिचय नाम :- मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख ( the Mathura Lion Capital Inscription ) स्थान :- मथुरा, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में यह लंदन के ब्रिट्रिश संग्रहालय में रखा है। भाषा :- प्राकृत लिपि :- खरोष्ठी समय :- प्रथम शताब्दी विषय :- शक महाक्षत्रप की शासनप्रणाली का ज्ञान, बौद्ध सम्प्रदाय सर्वास्तिवादी व महासंघिक का उल्लेख मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख : मूलपाठ प्रथम (क१) (१) महक्ष [ त्र ] वस रजुलस (२) अग्रमहेषि अयसिअ (३) कमु [ स ] अ धित्र (४) स्वर्र ( र्ह? ) ओस्तस युवरञ (५) मत्र नददि ( सि? ) अकस [ ए? ] (क२) (६) सध मत्र अबुहोल [ ए ] (७) पित्रमहि पिश्प्रस्त्रिअ भ्र- (८) त्र हयुअरन सध हन धि [ त्र ] (९) अतेउरेन होरक-प- (१०) रिवरेन इश्र प्रदूवि-प्रत्रे- (११) श्रे निसिमे शरिर प्रत्रिठवित्रो (१२) भक्रवत्रो शकमुनिस बुधस (१३) म ( ? ) किहि ( ? ) र ( त? ) य सश्प [ अ ] भुसवित ( ? ) (१४) ध्रुव च सधरम च चत्रु- (१५) दिवस सघस सर्व- (१६) स्तिवत्रन परिग्रहे [ ॥ ]१ (ग) (१) कलुइ-अ- (२) वरजो (घ) (१) नउलुदो [ । ] द्वितीय (ख) (१) महक्षत्रवस (२) वजुलस्य२ पुत्र३ (३) शुडसे क्षत्रवे४ (च१) (१) खर्र ( र्ह ) ओस्तो युवरय (२) खलमस कुमार (३) मंज कनिठ (४) समनमोत्र- (२) (१) क्र [ । ] करित ( ड, ढ़ ) ( १ ) अयरिअस (२) बुधत्रेवस (३) उत्रएन अयिमित ( स ? )- (झ१) (१) गुहविहरे (झ२) (१) धमदन ( ? ) (छ) (१) बुधिलस नक्ररअस (२) भिखुस सर्वस्तिवत्रस [ । ] (ज) (१) महक्ष [ त्र ] वस्य कुसुलअस पदिकस मेव ( ? ) किर (२) मियिकस क्षत्रवस पुयए [ ॥ ] (च३) (१) कमुइओ [ । ] तृतीय (ण) (१) क्षत्रवे शुडिसे (२) इमो पढ्रवि- (३) प्रत्रेश्रो (ट) (१) वेयउदिन कधवरो बसप- (२) रो कध- (३) वरो (४) वियउ- (ठ) (१) र्व……..पलिछिन ( ? ) (२) निसिमो करति नियत्रित्रो (३) सर्वस्तिवत्रन परि ( ? ) ग्रहे (त) (१) अयरिअस बुधिलस नकरकस भिखु- (२) स सर्वस्तिवत्रस पग्र- (३) न महसघिअन प्र- (४) म ( ? ) ञ-वित्रवे खलुलस ( ॥ ) (थ) (१) सर्वबुधन पुय [ । ] धमस (२) पुय [ । ] सघस पुय [ । ] (द) (१) सर्वस सक्रस्त (२) नस पुयए [ । ] (ध) (१) खर्दअस (२) क्षत्रवस [ । ] (न) (१) रक्षिलस (२) क्रोनिनस [ । ] (ठ१) (१) खलशमु- (२) शो [ । ] स्टेन कोनो इसके बाद खण्ड च रखते हैं जो यहाँ समूह २ में रखा गया है।१ रजुलस्य पढ़ा जाना चाहिए।२ स्टेन कोनो इसके बाद खण्ड य को रखते हैं।३ स्टेन फोनो इसके बाद खण्ड घ को रखते हैं।४ हिन्दी अनुवाद प्रथम ( क१) महाक्षत्रप राजुल की अग्रमहिषी, आयस कोमूसा की पुत्री; युवराज खरवस्त की माता, नददियक५ ने ( क२ ) अपनी माता आबुहोलिया, पितामही पिश्पस्पा, भाई हयुअरन के साथ, पुत्री हन [ और ] अन्त:पुर के होरक परिवार के साथ इस पृथ्वी प्रदेश में ( स्थान पर ) निःसीम ( स्तूप ) में भगवान् शाक्यमुनि बुद्ध का शरीर ( देहावशेष ) सबके मुक्ति निमित्त उत्थापित ( प्रतिष्ठित ) किया ………. ६ स्तूप और संघाराम को चारों दिशाओं के ( समस्त ) सर्वास्तिवादियों को प्रदान किया। ( ग ) कालुय्यवर [ और ] (घ) नवूलूद [ ने इसका निर्माण किया अथवा इसे लिखा ? ]। द्वितीय ( ख ) महाक्षत्रप राजुल पुत्र क्षत्रप शोडास [ आदेश करते हैं ] [ और ] ( च ) युवराज खरवस्त, कुमार खलामस, कनिष्ठ [ सबसे छोटे भाई ] मच इसका अनुमोदन करते हैं- ( ड, ढ़ ) आचार्य बुद्धदेव के शिष्य उदयन अजमित्र ( ? ) के ( झ ) गुहाविहार के धर्मदान को। ( छ ) सर्वास्तिवादिन भिक्षु नगर निवासी बुधिल को। ( ज ) महाक्षत्रप कुसुलक के पतिक के, मेनिक के, मियक के पूजा स्वरूप ( च३ ) कामूयिय [ ने इसको लिखा ? ]। तृतीय ( ण ) क्षत्रप शोडास [ आदेश देते हैं ] -इस प्रदेश में ( ट, ठ ) विजयोदीर्ण स्कन्धावार और पुसापुर स्कन्धावार [ में ] स्थित विजयोर्व…..परीक्षिण ( नामक पुरुष ) ने निःसीम ( स्तूप ) बनवाया और ( उसे ) सर्वास्तिवादियों को दिया ( त ) आचार्य नगर-निवासी भिक्षु बुधिल को प्रदान किया ताकि महासांधिकों को सत्य की शिक्षा दें७ ( थ ) सर्व बुद्ध की पूजा, धर्म की पूजा, संघ की पूजा। ( द ) सर्व-शक संस्थान की पूजा के निमित्त ( ध, न ) क्षत्रप खर्दक के, रक्षिल के और क्रोणिन के [ पूजा के लिए ]। (ठ १) खलमुख [ ने लिखा ? ]। स्टेन कोनो ने इसको इस प्रकार ग्रहण किया है-महाक्षत्रप राजुल की अग्रमहिषी, अवसिय कमुइया, युवराज खरोस्ट की पुत्री, नददियक की माता। इस अर्थ के प्रस्तुत करने में उनका तर्क यह है कि नददियक का नाम अग्रमहिषी से दूर है। किन्तु यह कोई तर्क नहीं है। संगत क्रम यही है कि पूर्व सम्बन्धियों का उल्लेख कर तब अपने नाम का परिचय दिया जाय।५ पंक्ति १३ का पाठ स्पष्ट नहीं है।६ इस पंक्ति का अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है।७ विश्लेषण क्रमबद्ध पंक्तियों के अभाव में लेख व्यवस्थित ढंग से नहीं पढ़ा जा सका है। यद्यपि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता, परन्तु प्रतीत होता है कि इसमें तीन स्वतन्त्र लेख हैं इसी रूप में विद्वानों ने मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख का अनुवाद प्रस्तुत किया है। प्रथम लेख से प्रकट होता है कि महाक्षत्रप राजुल ( रजुबुल ) की अग्रमहिषी ने अपने कतिपय सम्बन्धियों के सहयोग से बुद्ध के अवशेष पर स्तूप का निर्माण करवाया था। साथ ही यह भी प्रकट होता है कि स्तूप और संघाराम को उसने सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय को भेंटस्वरूप