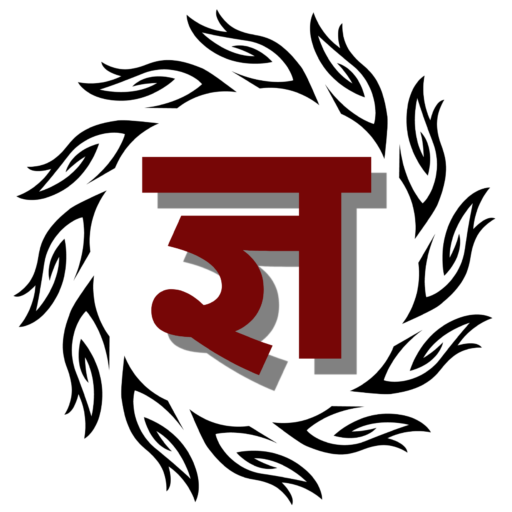भरहुत तोरण अभिलेख
भूमिका भरहुत तोरण अभिलेख मध्यप्रदेश के सतना जनपद में भरहुत नामक स्थान पर मिला है। इसकी खोज अलेक्ज़ेंडर कनिंगहम ने की। इनको यह एक विशाल स्तूप के ध्वंसावशेष मिले थे। उसके अधिकांश स्तम्भ, बाड़ आदि आजकल इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता में प्रदर्शित हैं। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें जो सबसे महत्त्व का माना जाता है वह एक तोरण पर अंकित है। यह लेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इसका समय कुछ विद्वान् ईसा पूर्व दूसरी शती मानते हैं। किन्तु दिनेशचन्द्र सरकार के मत में यह ईसा पूर्व प्रथम शती के उत्तरार्द्ध का है। इस लेख का महत्त्व इस बात में है कि इसमें उस प्रदेश के, जिसमें यह लेख प्राप्त हुआ है, कतिपय शासकों के नाम हैं। इस कारण मौर्योत्तर काल के प्रादेशिक इतिहास के निर्माण के लिए यह उपयोगी है। कुछ विद्वान इसे शुङ्ग वंश से सम्बद्ध मानते हैं। भरहुत तोरण अभिलेख : संक्षिप्त परिचय नाम :- भरहुत तोरण अभिलेख स्थान :- भरहुत, सतना जिला, मध्यप्रदेश लिपि :- ब्राह्मी भाषा :- प्राकृत विषय :- शुगकालीन निर्माण सम्बन्धी खोजकर्ता :- अलेक्ज़ेंडर कनिंघम भरहुत तोरण अभिलेख : मूलपाठ १. सुगनं१ रजे रञो गागी-पुतस विसदेवस २. पौतेण गोति-पुतस अगराजुस पूतेण ३. वाछि-पुतेन धनभूतिन कारितं तोरनां ४. सिला-कंमंतो च उपंण [ ॥ ] दिनेशचन्द्र सरकार ने इस उल्लेख से यह भाव ग्रहण किया है कि विश्वदेव विदिशा के उत्तरवर्ती शुङ्गों के अधीन शासक था। दूसरी ओर कनिंघम और राजेन्द्रलाल मित्र ने इसका तात्पर्य श्रुध्न राज्य ग्रहण किया था। अर्थात् दिनेशचन्द्र सरकार ‘सुगनं’ को शुङ्ग जबकि कनिंघम व राजेन्द्रलाल मित्र इसको श्रुध्न अनूदित करते हैं।१ अनुवाद [ शुङ्ग ] के राज्य में राजा गार्गीपुत्र विश्वदेव के पौत्र गोप्तीपुत्र२ अग्रराज३ के पुत्र वात्सीपुत्र-धनभूति द्वारा बनाया तोरण, शिला-कर्मान्त ( सम्भवतः ) बाड़ के स्तम्भ और उष्णीष४। कनिंगहम इसे कौत्सीपुत्र के रूप में ग्रहण करते हैं।२ दिनेशचन्द्र सरकार ने अगराजुस पढ़कर अङ्गारद्युत के रूप में उसका संस्कृतकरण किया है। उनका पाठ संदिग्ध लगता है। अग्रराज नाम अधिक संगत है। कनिंघम और राजेन्द्रलाल मित्र ने भी यही नाम ग्रहण किया है। इस नाम के राजा के अनेक सिक्के कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं और वे जर्नल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के अंकों में छपे हैं।३ दिनेशचन्द्र सरकार ने ‘उपंण’ का तात्पर्य ‘उत्पन्न’ ग्रहण किया है किन्तु यहाँ उसकी कोई संगति नहीं बैठती है।४ क्या पुष्यमित्र शुंग बौद्ध-द्रोही थे? ऐतिहासिक दृष्टि से इस लेख में शासक के रूप में कुछ व्यक्तियों की जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं जान पड़ती। किन्तु इसका महत्त्व तब हो जाता है जब कुछ विद्वान् प्रथम पंक्ति के आरम्भ के दो शब्दों का पाठ ‘सुगनं रजे’ स्वीकार कर उसमें शुङ्गों का उल्लेख देखते हैं। यदि वस्तुतः यहाँ तात्पर्य शुङ्ग राजाओं से है तो यह बात ध्यान देने की हो जाती है कि भारत के भरहुत स्तूप के इस तोरण को शुङ्गवंशी शासकों ने बनवाया था और इसके साथ शुङ्ग-वंश के संस्थापक पुष्यमित्र से सम्बद्ध धारणाओं को लेकर प्रश्न उभरता है। पुष्यमित्र द्वारा किये गये अश्वमेघों ( धनदेव का अयोध्या अभिलेख ) के आधार पर विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि उसके समय में ब्राह्मण-धर्म का पुनरुद्धार हुआ। वह ब्राह्मण-धर्म का प्रबल समर्थक था। इसके साथ ही कहा जाता है कि वह बौद्ध-धर्म द्वेषी था। इसके समर्थन के लिए विद्वानों ने दिव्यावदान, मंजुश्री-मूलकल्प और तारानाथ के इतिहास का सहारा लिया है। दिव्यावदान में कहा गया है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म का विनाश करने का निश्चय किया; कुक्कुटाराम विहार को ध्वस्त करने की चेष्टा की और शाकल में प्रत्येक श्रमण का सिर काटकर लाने के लिए १०० दीनार के इनाम की घोषणा की। मंजुश्री-मूलकल्प में गोमिमुख नामक राजा द्वारा स्तूप और विहारों को ध्वस्त करने और भिक्षुओं की हत्या करने का उल्लेख है। जायसवाल ने इस गोमिमुख को पुष्यमित्र के रूप में पहचानने की चेष्टा की है। तारानाथ के इतिहास से भी इसी तरह की बात पुष्यमित्र के लिए उद्धृत की जाती है। यदि ये कथन प्रामाणिक है५ तो ऐसे बौद्ध-धर्म-द्वेषी पुष्यमित्र के वंशजों द्वारा भारत में बौद्ध स्तूप का तोरण बनवाया जाना निःसन्देह एक असाधारण बात कही जायगी। अतः इस अभिलेख के प्रमाण से हेमचंद्र रायचौधरी६ सदृश विद्वान् शुंगों को उग्र ब्राह्मणवाद का नेता स्वीकार नहीं करते। वे यह मानते हैं कि पुष्यमित्र के वंशज रूढ़िवादी हिन्दू-धर्म के कट्टर माननेवाले भले ही रहे हों, परन्तु वे ऐसे असहिष्णु नहीं थे जैसा कुछ लेखकों ने चित्रित किया है। The Political and Socio-Religious Condition of Bihar – Dr. Hari Kishore Prasad५ Political History of Ancient India६ जो विद्वान्, पुष्यमित्र के बौद्ध-धर्म के प्रति कठोर दृष्टिकोण होने की बात में विश्वास करते हैं, उन्होंने बौद्ध-धर्म के प्रति सहृदयता के प्रतीक इस लेख को इस बात का द्योतक माना है कि पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों के समय यह भावनाएँ सम्भवतः कम हो गयी थीं और उन्होंने उदारता की नीति अपनायी थी। कुछ विद्वान् इस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं देखते जिससे ज्ञात हो कि उसका सम्बन्ध किसी प्रकार शुंगवंश के राजाओं से था। वे ‘सुगनं रजे’ का तात्पर्य मात्र शुंगों का राज्यकाल ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि तोरण के निर्माता शुंगवंश के नहीं थे। अतः इस लेख से शुंगवंश के धार्मिक विचारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती।