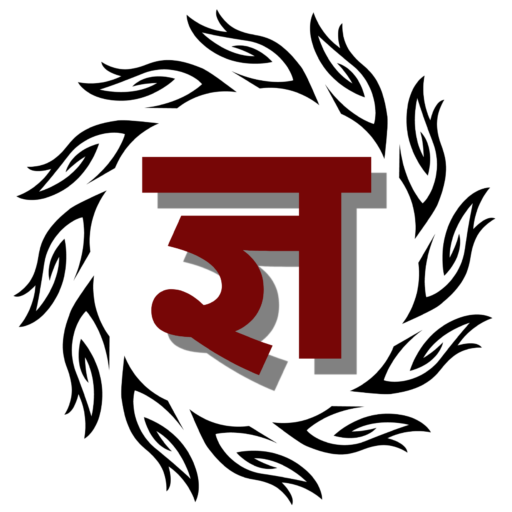नन्दपुर ताम्र-लेख; गुप्त सम्वत् १६९ ( ४८८ ई० )
भूमिका नन्दपुर ताम्र-लेख १६२९ ई० में कलकत्ता के गणपति सरकार को मुँगेर (बिहार) जिला अन्तर्गत सूरजगढ़ा से दो मील उत्तर-पूर्व नन्दपुर नामक ग्राम स्थित एक जीर्ण मन्दिर के ताक में जड़ा एक ताम्र- फलक मिला था। उसी पर यह लेख अंकित था। इसे न० ज० मजूमदार ने प्रकाशित किया। हाल में मजूमदार द्वारा व्यक्त विचारों […]
नन्दपुर ताम्र-लेख; गुप्त सम्वत् १६९ ( ४८८ ई० ) Read More »