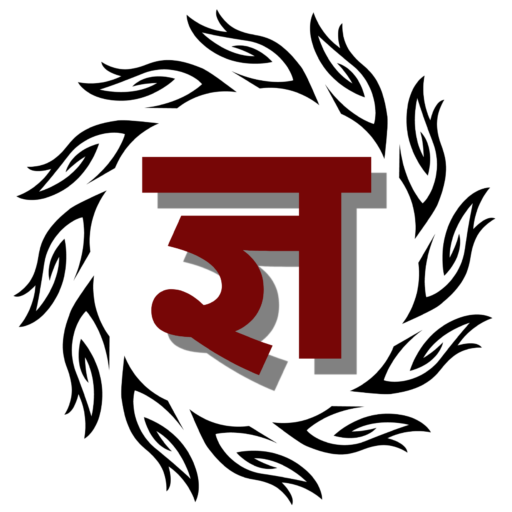ईश्वरसेन का नासिक गुहालेख
भूमिका ईश्वरसेन का नासिक गुहालेख लयण संख्या १० के आँगन के पश्चिमी दीवार पर अंकित है। अनुमान किया जाता है कि यह लेख १५ पंक्तियों का रहा होगा, परन्तु अब इसकी आरम्भिक १२-१३ पंक्तियाँ ही बच रही हैं; वे भी दाहिनी ओर क्षतिग्रस्त हैं। उसके कुछ अक्षर नष्ट हो गये हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखे इस अभिलेख के अक्षर सातवाहन अभिलेखों के बाद के जान पड़ते हैं। संक्षिप्त परिचय नाम :- ईश्वरसेन का नासिक गुहालेख ( Nasik Cave Inscription of Ishwarsen ) स्थान :- नासिक के गुहा संख्या १०, महाराष्ट्र भाषा :- प्राकृत लिपि :- ब्राह्मी समय :- आभीर नरेश ईश्वरसेन का ९वाँ राज्यवर्ष, ईश्वरसेन ने २४८-४९ ई० में कलचुरि-चेदि सम्वत् की स्थापना की अतः इस अभिलेख का समय २४७-२४८ ई० का है। विषय :- भिक्षुसंघ के लिए अक्षयनीवि दान का उल्लेख मूलपाठ १. सिधं [ । ] राज्ञः माढ़रीपुत्रस्य शिवदत्ताभीर पुत्रस्य २. आभीरस्येश्वरसेनस्य संवत्सरे नवमे ९ [ ग ]- ३. म्ह पखे चौथे ४ दिवस त्रयोदश १०+३ [ । ] [ एत ]- ४. या पुर्वया शकाग्निवर्म्मण: दुहित्रां गणपक [ स्य ] ५. रेभिलस्य भार्याया गणपकस्य विश्ववर्मस्य [ मा ]- ६. त्रा शकनिकया उपासिकया विष्णुदत्तया सर्वसत्त्व हि- ७. [ त ] सुखार्थ त्रिरश्मि पर्वत विहारवास्तव्यस्य [ चातुर्दिशस्य ] ८. भिक्षु संघस्य गिलान-भेषजार्थमक्षयनीवि प्रयुक्त [ गोवर्धनवास्त ]- ९. व्यास आगता [ नागता ] सु श्रेणिषु यतः कुलरिकश्रेण्या हस्ते कार्षापण १०. सहस्रं १००० ओदयंत्रिक सहस्रणि द्वे २ …. ११. [ ण्यां ] शतानि पंच ५०० तिलपिषक श्रे [ ण्याँ ] …… [ । ] १२. एते च कार्षापण चतालो [ पि ] ….. १३. ……..तस्य [ मास ] वृद्धतो …… हिन्दी अनुवाद १. सिद्धम्। शिवदत्त आभीर के पुत्र राजा माढ़रीपुत्र २. ईश्वरसेन आभीर के नवें संवत्सर के ३. ग्रीष्म के चौथे पक्ष का १३वाँ दिन। आज के दिन ४. शक अग्निवर्मा की दुहिता ( पुत्री ), गणपक ५. रेभिल की भार्या ( पत्नी ), गणपक विश्ववर्मा की माता ६. शकनिका उपासिका विष्णुदत्ता ने सर्व सत्त्वों के ७. हित और सुख [ प्राप्ति ] के निमित्त त्रिरश्मि पर्वत स्थित [ इस ] विहार में रहनेवाले चारों दिशाओं के ८. भिक्षुसंघ के भोजन ( गिलान ) और चिकित्सा की व्यवस्था के निमित्त [ गोवर्धन ] स्थित ९. वर्तमान और भावी श्रेणियों में [ निम्नलिखित ] अक्षयनीवि की स्थापना की- [ । ] कुलरिक श्रेणी में १०. कार्षापण, [ २ ] ओदयंत्रिक श्रेणी में दो हजार [ कार्षापण ]; [ ३ ] ……. श्रेणी में पाँच सौ कार्षापण ११. और [ ४ ] तिलपिशक श्रेणी में……[ कार्षापण ] [ । ] १२. इन चारों [ श्रेणियों ] को [ अक्षयनीवि के रूप में दिये गये ] कार्यापणों के १३. मासिक ब्याज से….. ईश्वरसेन का नासिक गुहालेख : महत्त्व ईश्वरसेन का नासिक गुहालेख इस बात की विज्ञप्ति है कि विष्णुदत्ता नाम्नी उपासिका ने गोवर्धन स्थित चार श्रेणियों के पास अक्षय-नीवि के रूप में कुछ धन राशि जमा कर इस बात का विधान किया था कि उस धन से प्राप्त होनेवाले ब्याज का उपयोग त्रिरश्मि पर्वतस्थित उस विहार में ( जिस विहार की दीवार पर यह लेख अंकित है ) रहने वाले भिक्षुओं के भोजन ( गिलान ) और चिकित्सा के लिए किया जाय। जिन चार श्रेणियों में अक्षय नीवि की स्थापना की गयी है, उनमें से केवल तीन का नाम उपलब्ध है। वे हैं; कुलरिक, ओदयंत्रिक और तिलपिशक। चौथी श्रेणी का नाम नष्ट हो गया है। तिलपिशक से निस्संदिग्ध अभिप्राय तेल पेरनेवाले लोगों की श्रेणी से है। कुलरिक को बहर ने कुलालों ( कुम्हारों ) की श्रेणी होने का अनुमान प्रकट किया है। जिस पहाड़ी में यह विहार है, उसमें स्थित एक अन्य गुहा-विहार ( गुहा संख्या १२ ) में कोलिक ( कौलिक ) निकाय का उल्लेख है। इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए भण्डारकर ने कुलरिक को कौलिकों ( जुलाहों ) की श्रेणी होने की कल्पना की है। इसी प्रकार ओदयंत्रिक के सम्बन्ध में सेनार्ट की धारणा है कि इसका आशय जल-यंत्र अथवा जल-घड़ी बनानेवाले कारीगरों से है। किन्तु हम इन मतों में से किसी से भी सहमत नहीं हैं। द्रष्टव्य है कि एक से अधिक श्रेणियों में अक्षयनीवि स्थापित करने के पीछे उपासिका विष्णुदत्ता की कोई निश्चित धारणा, भावना अथवा उद्देश्य रहा होगा। अक्षयनीवि सम्बद्ध अभिलेखों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि जिस कार्य के निमित्त किसी अक्षयनीवि की स्थापना की जाती थी, उसकी पूर्ति में सक्षम श्रेणी को ही धन देकर नीवि की प्रतिष्ठा की जाती थी। यह बात स्कन्दगुप्त कालीन इन्दौर अभिलेख देखने से स्पष्ट समझ में आ सकती है। उसमें सूर्य-मन्दिर में दीप जलाने की व्यवस्था की गयी है और इसके लिए धन राशि तैलिक श्रेणी को दी गयी है। ठीक उसी प्रकार इस अभिलेख में जिन चार श्रेणियों को धन दिया गया है, वे ऐसी ही श्रेणियाँ रही होंगी जिनका भोजन और भेषज ( चिकित्सा ) से सीधा सम्बन्ध है। अतः तिलपिशक श्रेणी को धन इसलिए दिया गया था कि वह तेल की व्यवस्था करे जो खाने तथा चिकित्सा दोनों के लिए आवश्यक था। ओदयांत्रिक श्रेणी का सम्बन्ध धान ( चावल ) कूटने अथवा आटा पीसनेवालों की श्रेणी से है। वे ही भोजन सामग्री प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकते थे। जल-यन्त्र अथवा जल-घड़ी बनानेवालों का प्रस्तुत प्रसंग में कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार कुलरिक श्रेणी भी कुम्हारों अथवा जुलाहों से भिन्न किसी वर्ग की श्रेणी रही होगी। अक्षयनीवि दात्री विष्णुदत्ता को शकनिका कहा गया है। अनेक अभिलेखों में ‘नारी’ के अर्थ में ‘निका’ प्रत्यय का प्रयोग देखने में आता है। यथा कुड़ा अभिलेख १, ९, १९ में विजया और विजयनिका का प्रयोग हुआ है। इस दृष्टि से शकनिका का भाव ‘शक जाति की स्त्री’ होगा। कहा जा सकता है कि इस शब्द का प्रयोग कदाचित यह बताने के लिए किया गया है कि वह शक नारी थी। यदि इस शब्द का यह उद्देश्य रहा हो तो यह निष्प्रयोजन पुनरुक्ति है क्योंकि उसके पिता अग्निमित्र को पहले ‘शक’ कहा जा चुका है। अतः डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त के अनुसार शकनिका का तात्पर्य यहाँ ‘शक नारी’ न होकर ‘शकनिक निवासिनी’ है। शकनिक सम्भवत: किसी स्थान का नाम है। विष्णुदत्ता के पति और पुत्र दोनों को अभिलेख में ‘गणपक’ कहा गया है। सामान्य रूप से इससे गण-प्रमुख का भाव ग्रहण किया जा सकता है और कहा जा सकता
ईश्वरसेन का नासिक गुहालेख Read More »