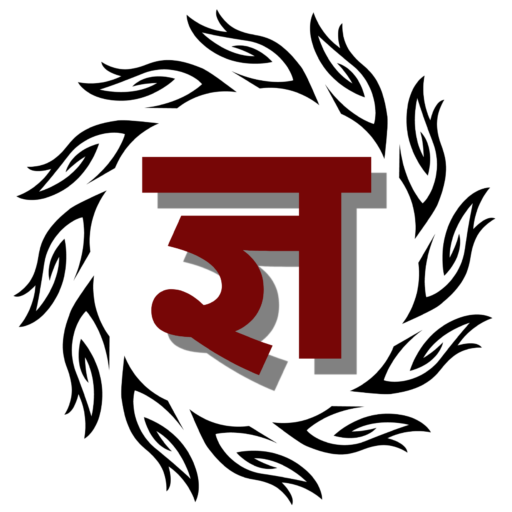चन्द्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख ( प्रथम )
परिचय उदयगिरि गुहा अभिलेख (प्रथम) मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जनपद में स्थित है। यह अभिलेख गुप्त सम्वत् वर्ष ८२ या ४०१ ई० का है। उदयगिरि विदिशा (मध्य प्रदेश) के उत्तर-पश्चिम कुछ ही दूर स्थित एक पहाड़ी है। उसके निकट ही एक गाँव है, जो इस पहाड़ी के कारण उदयगिरि कहा जाता है। इस उदयगिरि पहाड़ी के पूर्वी भाग में, गाँव के कुछ दक्षिण, धरातल पर ही एक गुहा-मन्दिर है। इस गुहा-मन्दिर में दो मूर्ति फलक हैं। एक में दो पत्नियों सहित भगवान विष्णु का और दूसरे में द्वादश-भुजी देवी का अंकन है। इन मूर्ति-फलकों के ऊपर लगभग २ फुट ४ इंच चौड़ा और १.५ फुट ऊँचा एक गहरा चिकना फलक है जिस पर यह लेख अंकित है। इस लेख को सर्वप्रथम एलेक्जेंडर कनिंघम ने १८५४ ई० में प्रकाशित किया था। १८५८ ई० में एडवर्ड थामस ने एच० एच० विलसन के अनुवाद के साथ अपना एक स्वतन्त्र पाठ प्रस्तुत किया था। तदनन्तर १८८० ई० कनिंघम ने इसे दुबारा संशोधित रूप में प्रकाशित किया। इसके पश्चात् फ्लीट ने इसको सम्पादित कर प्रकाशित किया। संक्षिप्त जानकारी नाम :- चन्द्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहाभिलेख (प्रथम) [ Udaigiri Cave Inscription of Chandragupta II ]। स्थान :- उदयगिरि, विदिशा जनपद; मध्य प्रदेश। भाषा :- संस्कृत। लिपि :- ब्राह्मी। समय :- गुप्त सम्वत् – ८२ या ४०१ ई० ( ८२ + ३१९ ), चन्द्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। विषय :- चन्द्रगुप्त द्वितीय के सामन्त सनकानिक महाराज द्वारा गुहादान। मूलपाठ १. सिद्धम्॥ संवत्सरे ८० (+) २ आषाढ़-मास-शुक्लेकादश्यां [ द ] परमभट्टारक महाराजाधि [ राज ] – श्री चन्द्र [ गु ] प्त-पादानुद्धयातस्य २. महाराज-छगलग-पौत्रस्य महाराज-विष्णुदास-पुत्रस्य सनकानिकस्य महा [ राज ] [ सोढ़ ] – लस्यायं देय-धर्म्मः। अनुवाद सिद्धि हो। संवत्सर ( वर्ष ) ८२ के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परमभट्टारक महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त के चरणों का चिन्तन करने वाले ( पादानुध्यात ) महाराज छगलग के पौत्र, महाराज विष्णुदास के पुत्र, सनकानिक महाराज [ सोढल ] का [ यह ] धर्म-दान [ है ]। ऐतिहासिक महत्त्व उदयगिरि गुहा अभिलेख ( प्रथम ) का कई दृष्टियों से महत्त्व है; जैसे – इसमें गुप्त सम्वत् का उल्लेख मिलता है, सनकानिक महाराज के उल्लेख है जोकि हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। सामान्य रूप में यह गुहा-निर्माण अथवा लेख के नीचे उत्कीर्ण मूर्ति फलकों के धर्म-दान के रूप में निर्माण कराये जाने की घोषणा है। यह धर्म-दान चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के एक सामन्त द्वारा दिया गया था। उसका नाम अभिलेख में स्पष्ट नहीं है; उपलब्ध संकेतों के आधार पर सोढल नाम की सम्भावना दिनेशचन्द्र सरकार ने प्रकट की है। भण्डारकर ने चार अक्षरों का नाम होने की सम्भावना व्यक्त किया है। उसने अपने को सनकानिक कुल (अथवा जाति) का बताया है। सनकानिक का उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की २२वीं पंक्ति* में सीमावर्ती जन-जाति के रूप में हुआ है। प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर अनेक विद्वानों की धारणा है कि सनकानिक लोग विदिशा के प्रदेश में रहते थे। किन्तु इस प्रकार की कल्पना इस कारण स्वयं असिद्ध है कि उन्हीं दिनों उसी प्रदेश में गणपति नाग का शासन था। समतट-डवाक-कामरूप-नेपाल-कर्तृपुरादि-प्रत्यन्त-नृपतिभिर्म्मालवार्जुनायन-यौधेय-माद्रकाभीर-प्रार्जुन-सनकानीक-काक-खरपरिकादिभिश्च-सर्व्व-कर-दानाज्ञाकरण-प्रणामागमन-* ( समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति – २२वीं पंक्ति )। चन्द्रगुप्त (द्वितीय) की पुत्री प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल में वाकाटक राज्य की व्यवस्था के लिये जो सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी पाटलिपुत्र से भेजे गये थे, उन्हीं में महाराज [ सोढल ] भी रहे होंगे। चन्द्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तम्भलेख ( Mathura Pillar Inscription of Chandragupta II )
चन्द्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख ( प्रथम ) Read More »