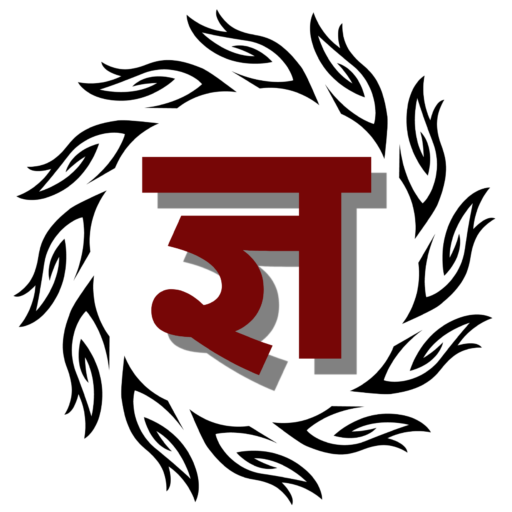भूमिका कनिष्क के १८वें राज्यवर्ष अर्थात् ९६ ई० का मणिक्याला अभिलेख रावलपिण्डी ( पाकिस्तान ) जिले के मणिक्याला नामक ग्राम से मिले स्तूप समूहों ( एक बड़े स्तूप तथा अनेक छोटे-छोटे स्तूपों तथा विहारों के अवशेष ) से १९३४ ई० में एक छोटे स्तूप के उत्खनन में दस फीट नीचे एक पत्थर पर अंकित मिला था जिसका प्रयोग वहाँ अस्थि-पेटिका के ढक्कन के रूप में हुआ था। यह अभिलेख खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा में है। मणिक्याला अभिलेख : संक्षिप्त परिचय नाम :- मणिक्याला अभिलेख ( Manikiala Inscription ) [ माणिक्याला / माणिक्याल / मणिक्याल / मणिक्यल ] स्थान :- मणिक्याला ग्राम, रावलपिण्डी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान भाषा :- प्राकृत लिपि :- खरोष्ठी समय :- ९६ ई० ( कनिष्क प्रथम के शासनकाल का १८वाँ वर्ष ) विषय :- बौद्धधर्म से सम्बंधित मणिक्याला अभिलेख : मूलपाठ १. सं १० [ + ] ४ [ + ] ४ कर्तियस मस [ स ] दिवसे २० [ । ] [ एत्र ] पुर्वए महरजस कणे- २. ष्क [ स्य ] गुषण-वंश-संवर्धक लल ३. दडणयगो वेश्पशिस क्षत्रपस ४. होरमु [ र्तो ] स तस अपनगे विहरे ५. होरमुर्तो एत्र णण भगव-बुद्ध-झुव ६. [ प्र ] तिस्तवयति सह तए [ न ] वेश्पशिएण खुदेचिए [ न ] ७. बुरितेण च विहरकर [ व्ह ] एण ८. संवेण च परिवरेण सध [ । ] एतेन कु- ९. शलमूलेन बुधेहि च ष [ व ] एहि [ च ] १०. समं सद भवतु ११. भ्रतर स्वरबुधिस अग्रप [ डि ] अशए १२. सध बुधिलेन नवकर्मिगेण [ ॥ ] मणिक्याला अभिलेख की पंक्तियाँ विभिन्न स्थलों पर अंकित हैं। प्रथम ६ पंक्ति मुख्य अंश में है। पंक्ति ७ से ९ बायीं ओर, पंक्ति १० ऊपर के बायें कोने में, पंक्ति ११ मुख्य लेख के ऊपर की ओर, पंक्ति १२ दायीं ओर पंक्ति २ के ऊपर अंकित है। हिन्दी अनुवाद संवत्सर १८ कार्तिक मास का दिवस २०। इस पूर्वकथित दिवस को महाराज कनिष्क के राज्य में। गुषण-वंश-संवर्धक, लल ( ? ) दण्डनायक, वेश्पसी के क्षत्रप, होरमूर्त१ और उनके आत्मज बिहार होरमुर्त। [ उन्होंने ] यहाँ तीन [ अन्य व्यक्तियों ] विश्वसिक खुदचियन्, बुरित और बिहरकर व्यएण तथा [ अपने ] परिवार के साथ भगवान् बुद्ध के अनेक स्तूप स्थापित किये। इनके [ इन स्तूपों के ] निर्माण का जो कुशलमूल ( पुण्य ) हो, ( उसमें ) बुद्धों, श्रावकों और अन्य लोगों के साथ भ्राता स्वरबुद्ध का मुख्य भाग हो। नवकर्मिक बुद्धिल के साथ। इसका एक अन्य अर्थ भी सम्भव है कुषाण वंश-संवर्धक लल, दण्डनायक वेश्पसी, क्षत्रप होरमूर्त। इस तरह इसमें तीन व्यक्तियों के नाम प्रतीत होते हैं। किन्तु आगे की पंक्ति में तीन अन्य व्यक्तियों के नामोल्लेख के परिप्रेक्ष्य में यहाँ तीन व्यक्तियों के नामों की सम्भावना नहीं है। पूरा वाक्य होरमूर्त का विशेषण ही प्रतीत होता है।१ मणिक्याला अभिलेख : विश्लेषण मणिक्याला अभिलेख स्तूप निर्माण सम्बन्धी सामान्य सूचना-पत्र है। इस प्रकार इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक विदेशी ने अभिलेख में उल्लिखित स्तूपों का निर्माण करवाया था। इससे बौद्ध धर्म के प्रति विदेशियों का आकर्षण प्रकट होता है। दानदाताओं के उल्लेख की दृष्टि से ही यह अभिलेख विशेष विचारणीय है। पंक्ति – ११ से ऐसा ज्ञात होता है कि जिसने इस अभिलेख को अंकित कराया, उसने अपने भाई होरमुर्त के पुण्य लाभ के लिए स्तूप बनवाये थे। उसने इस काम में तीन अन्य व्यक्तियों को सहयोगी बनाया था ( पंक्ति ६-८ )। उस व्यक्ति की चर्चा, जिसने स्तूप बनवाये और अभिलेख अंकित कराया, पंक्ति २-५ में है। यही विचारणीय अंश है। यह अंश इस प्रकार है — गुषण वंश-संवर्धक लल दडणयगो वेश्पशिस क्षत्रपस होरमुर्तो स तस अपनगे विहरे होरमुर्तो। स्टेन कोनो ने इसका अनुवाद ‘The general Lala, the scion of the Gushana race, the donation- master in his own Vihar’ किया है। इसका भाव है— दण्डनायक लल, गुषण-वंश की शाखावाला, क्षत्रप वेश्पसी का दानपति — वह अपने ही विहार में अपना दानपति है। इससे ऐसा प्रकट होता है कि अभिलेख और स्तूपों का निर्माता दण्डनायक लल था, वह गुषण वंश का था और क्षत्रप वेश्पसी का दानपति था और उसका अपना विहार था जिसका वह स्वयं ही दानपति था। इसमें दानपति ( Donation master ) शब्द का प्रयोग स्टेन कोनो ने होरमुर्त के लिए किया है। यह अनुवाद उन्हें लूडर्स ने सुझाया था। होर शब्द खोतानी-शक भाषा में दान ( gift ) के लिए प्रयुक्त पाया गया है। किन्तु पति के अर्थ में शक भाषा में मुर्त जैसा कोई शब्द नहीं है। स्वामी के अर्थ में मुरुण्ड शब्द मिलता है। उसी से यह शब्द निकला होगा ऐसा लूडर्स का अनुमान है। दानपति शब्द की कल्पना उन्होंने इसलिए की कि उन्हें तक्षशिला ताम्रलेख में महादानपति शब्द देखने को मिला था। यदि यह मान लिया जाय कि होरमुर्त का अभिप्राय दानपति है तो प्रश्न उठता है कि उसका यहाँ अभिप्राय क्या है? दानपति का अर्थ होता है — उदारदानी या महादानी — और ठीक इसी भाव में महादानपति का प्रयोग तक्षशिला ताम्रलेख में पतिक के लिए हुआ है। यहाँ ‘क्षत्रप वेश्पसी का दानपति’ कहा गया है। इस कथन से उदारदानी अथवा महादानी का भाव प्रकट नहीं होता है। इससे तो यह ज्ञात होता है कि यह कोई प्रशासनिक पद होगा। इस पदाधिकारी के जिम्मे राज्य की ओर से दान देने की व्यवस्था रही होगी। पर इस नाम के पदाधिकारी का परिचय किसी भी सूत्र से प्राप्त नहीं होता। यदि मान लें कि क्षत्रप वेश्पसी के यहाँ इस प्रकार का कोई पदाधिकारी था तो अभिलेख में दूसरी जगह ( पंक्ति ५ ) होरमुर्त की इस व्याख्या — वह अपने ही विहार में अपना दानपति था के स्पष्टीकरण की समस्या सामने उपस्थित होती है। विहारों में दान प्राप्त किया जाता था, दान दिया नहीं जाता था। वहाँ दान प्राप्त कर सुरक्षित रखनेवाले अधिकारी की आवश्यकता थी। निःसन्देह विहारों के इस अधिकारी का पदनाम ( designation ) राजकीय दान-व्यवस्थापक के नाम से भिन्न होना चाहिए। यह अकल्पनीय है कि दोनों पद एक ही नाम — होरमुर्त से पुकारा जाता रहा हो। अतः होरमुर्त से यहाँ किसी पद का अभिप्राय नहीं हो सकता है। होरमुज और होरमुरण्ड के रूप में होरमुर्द मथुरा के जमालपुर टीले से प्राप्त कई स्तम्भ लेखों में पाया गया है और वहाँ यह व्यक्तिवाचक नाम है। इन