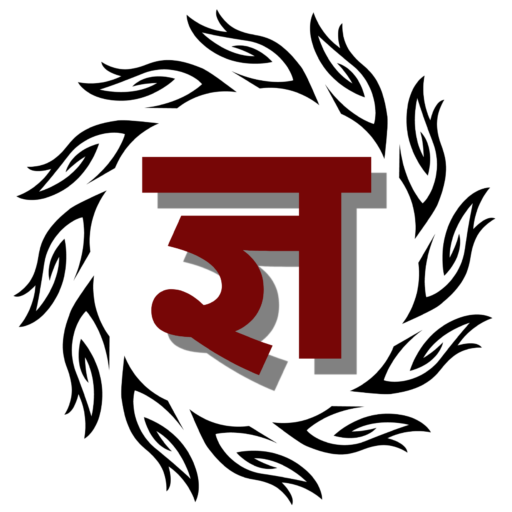भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर या तुलना
भूमिका एक जीवंत सभ्यता और संस्कृति का अपना विशिष्ट दर्शन होता है। ‘भारतीय दर्शन’ और ‘पाश्चात्य दर्शन’ का नामकरण भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है कि दोनों दर्शन एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। दर्शन की भाँति विज्ञान के क्षेत्र में हम ऐसा अन्तर नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में विज्ञान के सम्बन्ध […]
भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर या तुलना Read More »