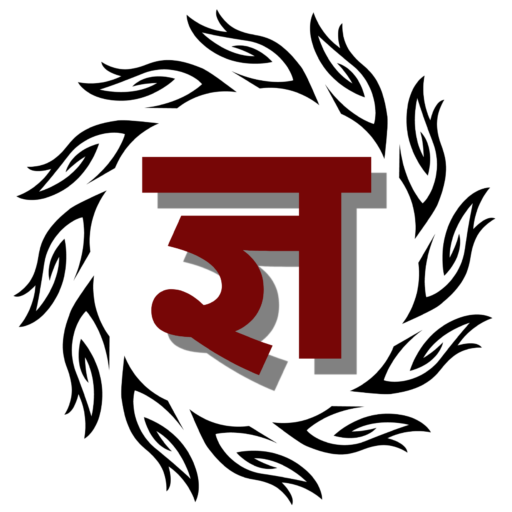धनदेव का अयोध्या अभिलेख
भूमिका अयोध्या से पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ किये जाने की जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख : संक्षिप्त विवरण नाम – धनदेव का अयोध्या प्रस्तर अभिलेख ( Ayodhya Stone Inscription of Dhandeva ) स्थान – अयोध्या जनपद उत्तर प्रदेश। भाषा – संस्कृत ( अशुद्ध प्राकृत प्रभावित )। लिपि – ब्राह्मी। समय – पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल ( द्वितीय शताब्दी ई०पू० ) विषय – पिता फल्गुदेय की मृत्यु पर पुत्र धनदेव द्वारा स्मारक की स्थापना। जिससे पुष्यमित्र के अश्वमेध की जानकारी मिलती है। मूल पाठ १ – कोलाधिपेन द्विरश्वजिनः सेनापतेः१ पुष्यमित्रस्य पष्ठेन२ कोशिकीपुत्रेण धन [ देवेन ]३ २ – धर्मराज्ञा४ पितुः फल्गुदेवस्य केतन५ कारित [ ॥ ] पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ का विवरण पतंजलि कृति महाभाष्य और कालिदास कृति मालिविकाग्निमित्र में भी हुआ है परन्तु यहाँ पर भी इसकी उपाधि ‘सेनापति’ ही मिलती है। यह परम्परा हम मध्यकाल में पेशवाओं के सम्बन्ध में देखते है। सिंहासन प्राप्त कर लेने के बाद भी वे पेशवा की उपाधि धारण करते रहे।१ इसका अभिप्राय है मातृपक्ष से पुष्यमित्र से छठे पीढ़ी में न कि पुष्यमित्र का छठा भाई। संस्कृत में इसके लिए ‘पुष्यमित्रित्’ का प्रयोग होना चाहिए परन्तु यह प्रयोग ‘पुष्यमित्रस्य’ पालि प्रभाव के कारण है।२ इसका पाठ कर सकते हैं — धनदेवन, धनदेन, धनकेन, धननन्दिना, धनभूतिना, धनमित्रेण, धनदत्तेन, धनदासेन इत्यादि। पिता नाम फलादेश होने से किन्तु पाठ ठीक प्रतीत होता है। धनदेवेन अयोध्या का स्थानीय शासक लगता है।३ पाठ – धर्मराजेन४ एक भवन या स्तम्भ ध्वज-स्तम्भ में फल्गुदेव की स्मृति में उसकी समाधि भूमि पर बना हुआ।५ हिन्दी रूपान्तरण १ – कोशल के राजा दो अश्वमेध यज्ञ करने वाले सेनापति पुष्यमित्र के छठे कोशिकी के पुत्र धनदेव द्वारा २ – धर्मराज पिता फल्गुदेव का निकेतन बनवाया गया। ऐतिहासिक महत्त्व अयोध्या अभिलेख जनपद ( उ० प्र० ) के अयोध्या से फैजाबाद जाने वाली सड़क पर अयोध्या से लगभग एक मील दूर बने रानोपाली भवन में बाबा सन्तबख्श की समाधि के पूर्वी द्वार के चौखट ललाट ( सिरदल ) से मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या अभिलेख यहीं उत्कीर्ण कराया हुआ मिट्टी में दबा होगा जिसे शिलापट्ट का प्रयोग पीछे अनजाने में इस चौखट में किया गया होगा। इसका उद्धार किसी इतिहास की दृष्टि पड़ने पर हुआ होगा। परन्तु अयोध्या अभिलेख कोशल के राजा धन ( देव ? ) द्वारा खुदवाया गया है जो पुष्यमित्र की पीढ़ी का है। इसमें ‘धन’ के बाद का भाग टूटा है पर इसके पिता का नाम यहाँ है। अतः उसके पुत्र का नाम धनदेव ही रहा होगा। इस नामधारी राजा के सिक्के अयोध्या से प्राप्त हुए हैं और बनारस के राजपाट की खुदायी से इस नाम के राजा की मुहरे भी मिली है। अब यह कल्पना कि धनमित्र, धनदत्त, धनदास अयोध्या के शासक थे के स्थान पर धनदेव नाम ही प्रामाणिक प्रतीत होता है। शुंग वंश के इतिहास में अयोध्या अभिलेख का विशेष महत्व है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें पुष्यमित्र की उपाधि सेनापति दी गयी है और उसके द्वारा किए जाने वाले दो अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है। साथ ही शुंग राजाओं की धार्मिक नीति तथा वंशपरम्परा पर भी इस प्रस्तर अभिलेख से प्रकाश पड़ता है। यह संस्कृत भाषा का दो पंक्तियों वाला लघु शिलालेख अत्यन्त उपयोगी है। कालिदास के माल्विकाग्निमित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस सन्दर्भ में उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को एक पत्र लिखा था जो यज्ञ के उद्देश्य को स्पष्ट करता है उसमें लिखा है – ‘स्वस्ति इस मण्डप से सेनापति पुष्यमित्र विदिशा में स्थित अपने पुत्र आयुष्मान अग्निमित्र को स्नेह से आलिंगन कर यह आदेश देता है — विदित हो राजसूय की दिशा के लिए मेरे द्वारा सैकड़ों राजपुत्रों से प्रवृत्त वसुमित्र की संरक्षता में एक वर्ष के भीतर लौट आने के विधान से यज्ञीय घोड़ा छोड़ा गया था। वह सिन्धु नद के दाहिने तट पर विचरता हुआ अश्वारोही सेना से युक्त यवन शासक द्वारा पकड़ा गया। इसके पश्चात् यवन सेना तथा वसुमित्र की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। धनुर्धर वसुमित्र ने शत्रुओं को विजित कर बलपूर्वक मेरा अश्वमेध का घोड़ा छुड़ा लाया। जिस प्रकार अंशुमान द्वारा लाए हुए थोड़े से उनके पिता महासगर ने यज्ञ किया था उसी प्रकार मैं भी यज्ञ करूँगा। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रसन्नचित होकर तुम्हें बहुओं के साथ यहाँ आना चाहिए।’ प्रस्तुत अभिलेख में भी पुष्यमित्र के लिए विशेषण प्रयुक्त है — ‘द्विरश्वमेधयाजिनः’ अर्थात् दो अश्वमेध यज्ञ करने वाला। इससे प्रमाणित होता है कि पुष्यमित्र ने दो अश्यमेधयज्ञ किया था जबकि माल्विकाग्निमित्र ( अंक – ५ ) से एक ही अश्वमेधयज्ञ का ज्ञान प्राप्त होता है जो यवनों को वहिष्कृत करने के लिए हुआ था पर यहाँ उल्लिखित दूसरे अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन स्पष्ट नहीं होता है। क्या हाथीगुम्फा अभिलेख का बहस्पतिमित्र और पुष्यमित्र शुंग एक ही थे? डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ने खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में उल्लिखित बहस्पतिमित्रि की समता पुष्यमित्र से मानकर खारवेल को पुष्यमित्र शुंग का समकालीन बताया है। उनके विचार में चूँकि पुष्यमित्र खारवेल से पराजित हो गया था अतः उसको अपनी प्रतिष्ठा के रक्षार्थ दूसरा अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था। डॉ० राजबलि पाण्डेय के अनुसार जायसवाल की यह प्रतिस्थापना बड़ी ही संदिग्ध है। उनकी दृष्टि में लिपिविज्ञान के आधार पर खारवेल के हाथीगुफा अभिलेख की तिथि पुष्यमित्र के समकालीन नहीं ठहरायी जा सकती। अतः खारवेल को पुष्यमित्र के समकालीन नहीं रखा जा सकता। उसके द्वारा पुष्यमित्र के समय मगध पर आक्रमण का प्रश्न ही नहीं उठता। पुनः हम यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार नक्षत्र और स्थानी की समता का प्रतिस्थापन कर डॉ जायसवाल ने पुष्यमित्र की समता हाथीगुम्फा अभिलेख में वर्णित वहस्पतिमित्र से स्थापित की है उससे लगता है कि यहाँ पूर्वाग्रहपूर्वक खींचा-तानी की जा रही हो या कोई ज्यामितिक हल निकाला जा रहा हो, जिसे सर्वथा मान्य नहीं ठहराया जा सकता। आगे हाथीगुम्फा अभिलेख के अध्ययन में यह देखेंगे कि वह अन्य प्रमाणों से भी पुष्यमित्र का समकालीन नहीं सिद्ध हो सकता। इसी से डॉ० पाण्डेय के मतानुसार यह “उसका दूसरा यज्ञ पूर्णार्थ ही था क्योंकि दूसरा अश्यमेधयज्ञ पूणार्थ होने का शास्त्रीय विधान है। अयोध्या अभिलेख : दो अश्वमेध यज्ञ डॉ० पुरुषोत्तम लाल भार्गव ने माना है कि पुष्यमित्र ने पहला
धनदेव का अयोध्या अभिलेख Read More »